Meera Bai श्री कृष्ण की प्रिय भक्त. जो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य उपासक थी. जिनका जीवन जुड़ा था प्रेम, त्याग और भक्ति से. जाने कृष्ण की भक्त मीरा बाई का इतिहास.
1. मीरा बाई का सामान्य परिचय | Meera Bai Parichay

क्या आपने कभी सोचा है, जब एक छोटी-सी बच्ची अपने नाना के महल की सीढ़ियों पर चढ़ती होगी, तो उसके मन में क्या उमंगें होती होंगी? शायद Meera Bai का जीवन भी कुछ ऐसा ही मासूम था। 1498 के आसपास राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जन्मी Meera Bai, अपनी मां को जल्दी खोकर महज तीन साल की उम्र में अपने नाना, मेड़ता के राव दूदा, के प्यार में पली-बढ़ी। लेकिन इस नन्ही उम्र में ही Mira Bai ने एक बड़ा फैसला लिया: कृष्ण की एक छोटी मूर्ति को अपने दिल का ‘पति’ मान लिया। सोचिए, वो छोटी सी बच्ची, उसकी मुस्कान और उसका दृढ़ निश्चय!
जब Meera Bai युवा हुईं, तो राजपरिवार ने उनके लिए एक ‘उचित’ शादी तय की—महाराणा सांगा के बेटे, भोजराज, से। दरबार में मीरा की कृष्ण भक्ति और राजसी परंपराओं के बीच टकराव की कहानी शुरू हुई। पत्नी के रूप में भोजराज ने उन्हें सम्मान दिया, लेकिन राजपरिवार की परंपराएं उनकी गहरी भक्ति को समझने में असफल रहीं।
1521 में भोजराज की युद्ध में मौत ने Meera Bai के दिल को और भी दुखी कर दिया। पति की याद में वे सती-प्रथा के खिलाफ अडिग रहीं; कहा जाता है कि उनके ससुराल वालों ने उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन मीरा ने हर बार अपने सच्चे प्रेम के साथ खुद को बचा लिया। उनकी मुस्कान के पीछे एक अटूट विश्वास था: “गोविंद बचा लेंगे।”
कई दुखों और सवालों के बाद, लगभग 1535 में, Meera Bai ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की राजसी दीवारों को अलविदा कहा। वे वृंदावन, मथुरा, पुष्कर और द्वारका जैसे पवित्र स्थलों की गलियों में खोजती रहीं—करूणा, प्रेम और आत्मसमर्पण का वह भाव, जो अब उनका जीवन बन चुका था। वृंदावन में गोस्वामी रूप-सनातन ने उन्हें ‘संत की सीढ़ी’ पर चढ़ते देखा; यहां सभी भेद मिट गए—नारी, पुरुष, राजसी—सब एकात्मक भक्ति के सामने फीके पड़ गए।
फिर आया उनका साहित्यिक कमाल: ‘मीरा-पदावली’। लगभग 1300 पदों में विरह का दर्द, माधुर्य रस की मिठास, और सामाजिक बंधनों पर Meera Bai का एक कोमल सवाल गूंजता है: “क्या प्रेम का रास्ता रूढ़ियों में बंध सकता है?” “मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई”—ये शब्द आज भी कानों में गूंजते हैं। उनकी सरल भाषा और लोकशैली में भावों की गहराई इतनी है कि हर दिल को छू जाती है।
जीवन की अंतिम कविता बनी उनका ‘समाधिस्थ होना’—द्वारका के बेट द्वारका मंदिर में, वर्ष 1547 (कुछ लोग 1563 मानते हैं) में कृष्ण मूर्ति में विलीन होने का जादू किया। कहते हैं, उस पल में कोई उत्तेजना नहीं थी—बस निरपेक्ष प्रेम का एक सौम्य विलय। आज भी जब कोई मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा होता है, तो मीरा की हंसी की गूंज मानो हवा में तैरती है।
Meera Bai ने हमें सिखाया कि भक्ति कोई रस्मी अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा का स्वाभाविक गीत है। उन्होंने रूढ़ियों की बेड़ियाँ तोड़ीं, कृष्ण को पति मानकर खुद को मुक्त किया, और अपनी कविताओं में प्रेम का प्रकाश फैलाया। पांच सौ वर्षों के बाद भी उनका गीत, उनकी मुस्कान, और उनका भरोसा हमारी आत्मा को जगाता है।
यह परिचय Meera Bai का नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का एक छोटा सा अंश है—जो हर मुसाफिर को कहता है: “चढ़ो, प्रेम की पगडंडी पर!”
2. मीरा बाई का विवाह
Meera Bai, भक्ति काव्य की एक अनमोल नायिका, का विवाह एक राजनीतिक समझौते के तहत हुआ, लेकिन इसने उनके आंतरिक जीवन को भी नई दिशा दी। 1516 में, उन्हें मेड़ता के राठौड़ परिवार से उठाकर मेवाड़ के युवराज भोजराज सिसोदिया के साथ शादी के बंधन में बांध दिया गया। इससे मारवाड़ और मेवाड़ के दो शक्तिशाली राजवंशों का गठजोड़ और मजबूत हुआ।

1 की रस्म और कृष्ण‑प्रेम
जब Meera Bai बारह-तेरह साल की थीं, तब उन्होंने विवाह की रस्म के दौरान अपने हाथों में गोपाल की एक छोटी सी मूर्ति थाम रखी। फेरे लेते समय उन्होंने कहा, “मैंने तो चिर दूल्हा चुन लिया।” भोजराज इस अनोखी बात से थोड़े चकित हुए, लेकिन उन्होंने मीरा के लिए महल में एक निजी कृष्ण मंदिर बनवाकर उनके इस प्रेम को मान्यता दी। उस समय किसी राजमहल में ऐसी छूट पाना बहुत मुश्किल था।
2 शाही महल में सहमति और टकराव
शुरुआत के सालों में Meera Bai और भोजराज के बीच एक दोस्ताना रिश्ता पनपा। भोजराज मीरा के भजन सुनकर बहुत खुश होते और उनका आत्मविश्वास बढ़ाते। लेकिन मीरा की सास, ससुर और ननद उदाबाई को यह बात पसंद नहीं आई कि एक महिला का “कृष्ण पति” होना राजपूत मर्यादा के खिलाफ है। वे मीरा को कुल देवी दुर्गा की पूजा और गंगौर व्रत में शामिल करना चाहते थे, लेकिन मीरा ने साफ मना कर दिया। उदाबाई ने भोजराज से यह तक कह दिया कि मीरा किसी और से प्रेम करती हैं, लेकिन जब सच सामने आया, तो भोजराज ने अपनी बहन को डांटकर मीरा की रक्षा की।
3 विधवापन और सामाजिक कसौटी
1521 में, भोजराज युद्ध में घायल होकर चल बसे, जिससे Meera Bai की सुरक्षा की परत भी हट गई। राजपरिवार ने उन पर सती होने का दबाव डाला, लेकिन मीरा ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। उनके लिए “पति धर्म” अब भी गिरधर ही थे। कहा जाता है कि उन्हें मारने की कई कोशिशें हुईं, जैसे विष पीने के लिए भेजना, लेकिन हर बार “सच्चे प्रेम” ने उनकी रक्षा की।
4 वैवाहिक अनुभव की धरोहर
भोजराज का प्यार और दरबारी प्रतिरोध, दोनों ने मिलकर Meera Bai की भक्ति को और मजबूत किया। महल की सोने-चांदी ने जब उन्हें जकड़ने की कोशिश की, तो कृष्ण का नाम उन्हें आज़ादी दी। यही संघर्ष उनके भजनों को दिल को छू लेने वाला बनाता है। “मेरे तो गिरधर गोपाल…” जैसे पदों में पति का वियोग, नारी की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक प्रेम सब एक साथ झलकते हैं। ये स्वर उसी विवाह के अनुभव की हल्की आंच पर पककर लोक अनुभव की सुगंध बन गए हैं।
मीरा बाई का विवाह सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है; यह एक ऐसा पुल है जहां राजदरबार की औपचारिकता, मानवीय प्रेम की नमी और अनंत भक्ति का सूर्योदय एक साथ मिलता है। यह एक ऐसी कहानी है, जो पांच सदियों बाद भी पाठकों और श्रोताओं के दिल को छू लेती है।
3. संत मीरा बाई की नीतियां
Meera Bai की “नीति” असल में उनके जीवन के दर्शन का एक हिस्सा थी। यह एक ऐसी सरल और भावुक भाषा थी जो प्रेम को धर्म, इंसान को मंदिर, और अंतरात्मा को गुरु मानती थी। यहां उनके पांच मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताया गया है, जो न केवल विचार हैं, बल्कि उनके जीवन के संघर्षों की कहानियां भी हैं।
1. एकनिष्ठ और जीवंत कृष्ण-भक्ति
मीरा ने अपने बचपन में जो श्याम-मूर्ति देखी, उसे ही उन्होंने “अमर पति” माना और अपने जीवन भर उसी से बात की। उनके पदों में भगवान कोई दूर की चीज नहीं, बल्कि एक प्रियतम मित्र की तरह हैं। इससे भक्ति का अर्थ सिर्फ कर्मकांड नहीं रह जाता, बल्कि यह एक गहरा दिल का रिश्ता बन जाता है।
2. व्यक्तिगत अनुभव पहले, रीति-रिवाज बाद में
उन्होंने साफ कहा, “राम-नाम रस पीजै, पण्डित पूजा धरि।” उनके लिए बाहरी यज्ञ-जप से ज्यादा महत्वपूर्ण था ‘भीतर का प्रेम’। इसी वजह से उन्होंने मंदिर के पुरोहितों और पंडितों की मध्यस्थता को नकारा और हर भक्त को सीधी राह दिखाई।
3. जाति और लिंग की दीवारें तोड़ना
राजपूत राजकुमारी होते हुए भी Meera Bai ने संत रविदास जैसे दलित गुरु को अपनाया, जो उस समय की ब्राह्मणवादी सोच को चुनौती देता था। उनकी कविताएं इस बात को दर्शाती हैं कि प्रेम में “ना घर मेरा, ना घर तेरा” है, यानी ईश्वर सबका है। इसलिए, उन्होंने स्त्रियों और निचली जातियों के लिए भक्ति का एक ऐसा मार्ग खोला जो स्वागत का प्रतीक बन गया।
4. सामाजिक रूढ़ियों से निर्भीक असहमति
पति भोजराज की मृत्यु पर सती होने से मना कर उन्होंने स्त्री-स्वातंत्र्य का एक नया स्वरूप पेश किया। इस दौरान उनके ससुराल ने उन्हें विष भेजा और सांप भेजे, लेकिन उन्होंने “सच्चे प्रेम” के भरोसे सब सह लिया और एक चलती-फिरती चुनौती बन गईं।
5. साधारण जीवन, करुणा और मानवता
Meera Bai ने महलों को छोड़कर साधुओं और गरीबों के बीच रहना चुना। उनकी पंक्ति “अमीर के छप्पन भोग फेंक दो, नमक-रोटी ही सच्ची” शोषण के खिलाफ एक सीधा वार है। उनका भक्ति-योग सेवा और स्मरण को जोड़ता है—देवता की पूजा तब पूरी मानी जाती है, जब दुखियों के आँसू पोंछे जाएं।
मानवीय पक्ष की गूँज
इन सिद्धांतों में एक गहरी मानवीय भावना है:
- प्रेम को नियमों से बड़ा मानने के कारण वे नारीवादी क्रांतिकारी भी बनती हैं, लेकिन वे कभी कठोर नहीं हुईं। वे गाती रहीं, “मेरे तो गिरधर गोपाल…” और कठोर दिलों को भी पिघलाती रहीं।
- उनका आत्म-विश्वास इस बात पर आधारित था कि “मैं समाज से नहीं, अंतरात्मा से उत्तरदायी हूँ।”
आज के लिए संदेश
Meera Bai की नीतियाँ आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। वे हमें सिखाती हैं कि आध्यात्मिकता मंदिरों या वंश के मान-सम्मान से नहीं, बल्कि उस कोमल स्थान से आती है जहां इंसान और ईश्वर दोनों प्रेमी बन जाते हैं। इस प्रेम में न जाति की बात होती है, न लिंग की, न धन की; बस दिल की खिड़की खुली होनी चाहिए। यही मीरा की नीति का मूल मंत्र है—निर्भीक प्रेम, निष्कपट सेवा और सभी के प्रति समान दृष्टि।
4. मीरा बाई की रचनाएं
संत Meera Bai की रचनाएँ लगभग पाँच शताब्दियों पुरानी हैं और इनमें उनकी आत्मकथा का एक पारदर्शी रूप देखने को मिलता है। इन पक्तियों में कृष्ण के प्रति उनका गहरा प्रेम, सामाजिक विद्रोह और स्त्री‑स्वतंत्रता की भावना एक साथ गूंजती है। अध्ययन के अनुसार, 100 से 200 पद मीरा की मौलिक रचनाएँ मानी जाती हैं, जबकि मौखिक परंपरा के अनुसार, वे 1,300 से अधिक भजनों का स्रोत हैं।
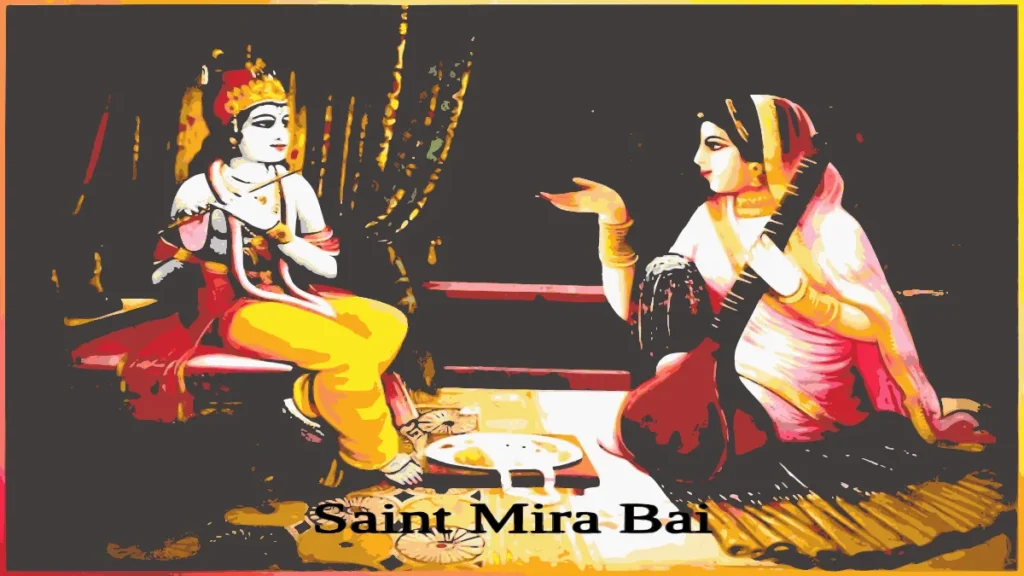
1. भाषा, छंद और संरचना
इन पदों का संग्रह “मीरा‑पदावली” के नाम से विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों और आधुनिक संपादित संस्करणों में सुरक्षित है। Meera Bai ने राजस्थानी, ब्रज‑भाषा और गुजराती का एक सहज मिश्रण करते हुए लगभग 6-8 पंक्तियों के पद लिखे। इनमें प्रायः मात्रिक छंद होता है और हर पद के साथ राग का संकेत भी मिलता है, जैसे मीरा‑की‑मल्हार और राग सोरठा। उनकी सरल भाषा और दोहराव से भरे टेक्स्ट ने इन्हें लोकगीत जैसा बना दिया, जिससे ये साहित्य गाँव के चौपाल से लेकर शास्त्रीय मंच तक पहुँच गए।
2. पदावली की प्रमुख कृतियाँ
उनकी कुछ प्रमुख कृतियों में “पायो जी मैंने राम‑रतन धन पायो” शामिल है, जो कृष्ण‑भक्ति के आनंद को दर्शाता है। इसे पहले डी.वी. पालुस्कर और फिर लता मंगेशकर ने गाकर लोकप्रिय बनाया। “मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई” भी एक ऐसा पद है जो विरह की व्यथा और पूर्ण समर्पण को व्यक्त करता है। कम प्रसिद्ध लेकिन कलात्मक “मन थें परस हरि रे चरण” पद Meera Bai के भक्ति‑दर्शन का एक सुंदर उदाहरण है, जिसमें राग तिलंग का साथ है। उनकी रचनाओं में स्तुति, विरह‑वर्णन, प्रेम‑उल्लास और सामाजिक व्यंग्य जैसे चारों रस एक साथ मिलते हैं।
3. और “ह्यूमन टच”
Meera Bai की कविता में “मानव” और “दैवी” के बीच कोई कठोर विभाजन नहीं है। वे कृष्ण को अपने सखा‑शील पति के रूप में और खुद को दासी‑प्रेयसी के रूप में चित्रित करती हैं। जैसे कि “तन मन गिरधर के संग लगाए, जगत रीत सब झूठी” पंक्ति में सांसारिक माया पर करुण टिप्पणी की गई है। उनके पदों में अक्सर घरेलू प्रसंग जैसे सास का उलाहना और ननद की चुभन भी मिलते हैं, जिससे एक आम स्त्री का दर्द और जिजीविषा कविता का हिस्सा बन जाती है।
4. —राग और गायकी
Meera Bai की राग‑परंपरा में मीरा‑की‑मल्हार और मीरा‑की‑मंझ जैसी शैलियाँ उनके नाम से जानी जाती हैं। इन भजनों को हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों शास्त्रीय घरानों ने स्वीकार किया है। आज भी मीरा के पद कथक, भारतनाट्यम और सूफ़ी मंचों पर नृत्य‑भाव के साथ गूंजते हैं। राग‑रूप, लयबद्ध टेक और सरल ताल ने लोक‑भक्ति और शास्त्रीय वैभव के बीच एक पुल बना दिया है।
5. प्रामाणिकता और पांडुलिपि‑संकट
हालांकि, मीरा के जीवनकाल की कोई मूल पांडुलिपि उपलब्ध नहीं है। सबसे प्राचीन दो पद 18वीं सदी के संग्रह में मिलते हैं। इसीलिए कुछ विद्वान, जैसे जॉन स्ट्रैटन हॉली, चेताते हैं कि आज के पदों में कुछ “लोक‑हस्तक्षेप” हो सकता है। फिर भी, रचनाओं की शैलीगत संगति—जैसे माधुर्य‑रस, संक्षिप्त पंक्तियाँ और गिरधर‑स्मरण—मीरा की पहचान बनाने में मदद करती है।
6. आधुनिक पुनर्पाठ और अनुवाद
आधुनिक संपादकों, जैसे आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, ए.जे. ऑल्स्टन और वी.के. सुब्रमणियन, ने मीरा के पदों के आलोचनात्मक संस्करण और अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किए हैं। इससे वैश्विक पाठकों के बीच मीरा की पहुँच संभव हुई है। फ़िल्म “प्रेम रतन धन पायो” से लेकर जॉन हर्बिसन के “Mirabai Songs” तक, उनकी पंक्तियाँ नए सांस्कृतिक संदर्भ रचती रहती हैं।
5. मीरा बाई ओर तुलसी, सुर, कबीर जैसे भक्तो के बीच संबंधों की व्याख्या
संत मीरा बाई, तुलसीदास, सूरदास और कबीर—इन चारों ने 15-16वीं शताब्दी के उत्तर-भारतीय भक्ति आंदोलन को अलग-अलग आवाज़ों से एक ही सुर में पिरोया। मीरा और सूर की कृष्ण-भक्ति, तुलसी का राम का मार्ग और कबीर का निर्गुण प्रेम—ये तीनों धाराएँ मिलकर समाज में ऊँच-नीच, स्त्री-बंधन और सांप्रदायिक दीवारों पर करुणा, सरलता और विद्रोह का रंग चढ़ाती रहीं।
इतिहास की कहानियाँ बताती हैं कि ये संत सिर्फ युगसाथी ही नहीं थे, बल्कि उनके बीच विचारों का आदान-प्रदान भी हुआ। कहीं-कहीं तो उनके बीच प्रेरक पत्रों का भी लेन-देन हुआ, जैसे वृंदावन में उनकी आत्मीय भेंटें। उनके रिश्तों को समझना दरअसल भक्ति-युग के गहरे अर्थ को जानने जैसा है।
5.1 काल-परिस्थितियाँ और निकटवर्ती जीवन-रेखाएँ
कबीर (1440-1518) भक्ति-लहर के शुरुआती प्रतीक थे; मीरा (1498-1547), सूरदास (1478-1583) और तुलसीदास (1511-1623) उनकी परवर्ती पीढ़ियाँ हैं। इनका अधिकांश जीवन मुग़ल काल में एक-दूसरे के समकाल पर बीता। उनके overlapping वर्ष इस बात की संभावना को मजबूत करते हैं कि उनकी रचनाएँ और परंपराएँ एक-दूसरे से प्रभावित थीं।
5.2 भावधाराओं का संगम: सगुण और निर्गुण
कबीर ने निर्गुण उपासना के जरिए मूर्तिपूजा और कर्मकांड पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहार।” मीरा, सूर और तुलसी ने सगुण प्रेम में खुद को डुबोया, लेकिन कबीर की समानता-भाषा से वे अलग नहीं हुए। मीरा के भजनों में भी जाति-भेद के खिलाफ आवाज़ उठती है। सगुण-निर्गुण का यह द्वंद्व भक्ति आंदोलन की जीवंत चर्चा बना, जिसे आज के विद्वान ‘सांस्कृतिक संवाद’ के रूप में पहचानते हैं।
5.3 साहित्यिक आदान-प्रदान और जनश्रुति
मीरा-तुलसी संवाद
एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार, Meera Bai ने चित्तौड़ से निर्वासित होने पर तुलसीदास को पत्र लिखकर आध्यात्मिक मार्गदर्शन मांगा। तुलसी ने उन्हें “धीरज धर” कहकर कृष्ण की भक्ति में अडिग रहने की सलाह दी। यह कहानी भले ही किंवदंती लगे, लेकिन दोनों की रचनाओं में स्त्री-स्वातंत्र्य और भक्ति की समानता दिखती है। वृंदावन के कुछ मंदिरों में कहा जाता है कि मीरा और तुलसी ने एक साथ ठाकुर जी के चरण छुए, तभी से भक्तों को प्रतिमा स्पर्श की अनुमति मिली।
मीरा-सूर निकटता
सूरदास की कृष्ण-लीला और Meera Bai का प्रेम-विरह, दोनों ब्रज-भाषा में रचे गए थे। वल्लभाचार्य परंपरा सूर को ‘अष्टछाप’ कवियों में गिनती है, जहाँ मीरा के भजन भी गाए जाते हैं। लोककथाएँ कहती हैं कि अंधे सूर ने वृंदावन में मीरा की आवाज़ पहचानते हुए कहा—“यह तो वही प्रेम है जिसे सुनने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं।” दोनों ने ब्रज को काव्य-भाषा का मान दिलाया, जिस पर आज के आलोचक एकमत हैं।
कबीर की छाया
मीरा को संत रविदास की शिष्या माना जाता है; रविदास रामानंद-कबीर परंपरा के थे, जिससे मीरा पर निर्गुण प्रेम की छाप पड़ी। कबीर के “जाति न पूछो साधु की” के दृष्टिकोण को मीरा ने अपनी स्त्री-स्वतंत्रता की पुकार में व्यक्त किया। तुलसी ने भी अवधी रामकथा के जरिए इसे आम भाषा में फैलाया।
5.4 साझा विरासत और आज का अर्थ
इन चार संतों का संबंध कोई औपचारिक ‘संघ’ नहीं था, बल्कि यह अनुभवों से भरा एक जाल था—भाषा की सरलता, ईश्वर-प्रेम और सामाजिक आलोचना के तंतु, जिन्हें उन्होंने एक-दूसरे से सींचा। कबीर ने सवाल उठाने की प्रेरणा दी, सूर और मीरा ने प्रेम में डूबने का सिखाया, और तुलसी ने धर्म और नीति को कथा में पिरोकर आम लोगों तक पहुँचाया।
आज भी मंदिरों में मीरा और सूर के भजन, रामलीला में तुलसी के दोहे और लोकगीतों में कबीर के दोहे एक साथ सुनाई देते हैं, जैसे कि पाँच शताब्दियों बाद भी उनका संबंध हमारी सांस्कृतिक धड़कनों में एक ही धुन गा रहा हो।
6. मीरा बाई का इतिहास | Meera Bai History

6.1 केसे बीता मीरा बाई का बचपन | Meera Bai
Meera Bai का बचपन एक अनोखे संगम का उदाहरण था, जहां राजसी वैभव और गहरी भक्ति दोनों का मिलन हुआ। उनका जन्म 1498 के आसपास मारवाड़ के कुड़की (मेड़ता) में राठौड़ राजपरिवार में हुआ। जब मीरा सिर्फ चार या पांच साल की थीं, तब उनकी माँ वीर कुँवरि का निधन हो गया। इसके बाद, उनके नाना राव दूदा ने उन्हें मेड़ता के किले में पाला।
किले का माहौल पूरी तरह से विष्णु भक्ति से भरा हुआ था। दादाजी की निजी सभा में रोज़ भागवत कथाएँ और कृष्ण लीलाएँ सुनाई देती थीं। एक दिन, जब Meera Bai ने बारात को गुजरते देखा, तो उन्होंने अपनी माँ से मासूमियत भरा सवाल किया, “मेरा दूल्हा कौन होगा?” माँ ने पास रखी श्याम मूर्ति की ओर इशारा किया, और उसी पल से कृष्ण उनके “अमर पति” बन गए। कुछ कहानियाँ बताती हैं कि संत रैदास या एक साधु ने उन्हें पांच साल की उम्र में एक छोटी कृष्ण की मूर्ति भेंट की।
Meera Bai उस मूर्ति को नहलाती, सजाती, उससे बातें करती और मधुर गान गाती थीं। एक राजकुमारी होने के नाते, उन्हें शस्त्र विद्या, तीरंदाजी, घुड़सवारी और शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण मिला, लेकिन उनके दिल में हमेशा भक्ति का ही गाना गूंजता रहा।
सुबह होते ही वे किले की बालकनी से सूरज को उगते हुए देखकर कृष्ण की स्तुति गुनगुनाती थीं। दोपहर में गुरुजनों से वेद और पुराण पढ़ते-पढ़ते हवेलियों की गलियों में गाते हुए घूम जातीं। शाम को राव दूदा की सभा में साधु-संतों के बीच बैठकर वे आध्यात्मिक चर्चाएँ सुनतीं, जैसे हर शब्द में कृष्ण का नाम खोज रही हों।
इस तरह, उनके बचपन ने Meera Bai के भीतर यह विश्वास पैदा किया कि राजकुमारियाँ भी अपने मन की राह चुन सकती हैं, और उनकी राह थी निस्सीम प्रेम। यही अनुभव बाद में उनके भजनों की आत्मा बन गया, जिसने सदियों से लोगों के दिलों को छुआ है।
6.2 संत मीरा बाई की श्री कृष्ण के प्रति भक्ति
Meera Bai की भक्ति कोई साधारण पूजा नहीं थी; यह तो उस गहरे प्रेम की अभिव्यक्ति थी, जिसने एक राजकुमारी को “गिरधर गोपाल” का साथी बना दिया। उन्होंने हर मुश्किल में अपने भगवान पर भरोसा रखा।
बचपन में एक साधु ने उन्हें एक छोटी सी कृष्ण की मूर्ति दी। Meera Bai ने उसे अपना पति मान लिया और उसके साथ खाना-पीना तक शुरू कर दिया, जैसे वह सच में उनके साथ हो। राजमहल की बालकनी से सूर्योदय का नजारा देखते हुए, वे उससे बातें करतीं और अपने पहले भजन लिखने लगीं।
जब वे बड़ी हुईं, तो उन्हें विवाह, दरबार और सैन्य शिक्षा का भव्य जीवन मिला, लेकिन उनके दिल में बस यही गाना गूंजता रहा: “मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई।” उनका काव्य ब्रज-भाषा में इतना मधुर हो गया कि वह लोकगीत बन गया।
भक्ति की परीक्षा भी कम कठिन नहीं थी। ससुराल वालों ने उन्हें विष का प्याला, सांपों से भरी टोकरी और कीलों वाली बिस्तर भेजी, लेकिन जब उन्होंने प्रार्थना की, तो वह प्याला अमृत बन गया, सांप शालिग्राम में बदल गए और कीलें फूल बन गईं। इन चमत्कारों ने न केवल Meera Bai का विश्वास मजबूत किया, बल्कि लोगों को यह संदेश दिया कि सच्चा प्रेम ही भगवान की रक्षा है।
आखिरकार, द्वारका के मंदिर में उन्होंने मूर्ति से लिपटकर देह त्याग दिया। कहा जाता है कि वे श्याम-प्रतिमा में विलीन हो गईं, ताकि प्रेम और प्रियतम कभी जुदा न हों।
Meera Bai की भक्ति हमें यह सिखाती है कि ईश्वर से निजी संवाद में जाति, लिंग, रीति-रिवाज या डर कोई बाधा नहीं होते। जब प्रेम सच्चा और निडर हो, तो विष भी प्रसाद बन जाता है।
6.3 मीरा बाई का भक्ति आंदोलन में योगदान
Meera Bai ने भक्ति आंदोलन में अपनी आत्मा को पूरी तरह से समर्पित किया और साथ ही समाज की कठोर बंदिशों को भी तोड़ने का काम किया। एक राजकुमारी से संत बनने वाली मीरा ने पुरुष-प्रधान धर्मशास्त्र को चुनौती दी। जब उनके पति भोजराज का निधन हुआ, तो उन्होंने सती प्रथा को अपनाने के बजाय “गिरधर गोपाल” को अपना एकमात्र साथी मान लिया। इस साहसिक कदम ने महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए एक नया अध्याय लिखा।
उनकी भावनाओं से भरी रचनाएँ, जो ब्रज-भाषा और राजस्थानी का खूबसूरत मिलाजुला रूप थीं, गांव-गली में हर किसी तक पहुँच गईं। जैसे कि “मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई” जैसे भजन लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते थे और मंदिरों से बाहर निकलकर हर जगह गूंजने लगे। इस संगीत ने भक्ति को सिर्फ विद्वानों और दरबारी पुरोहितों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे आम लोगों के दिलों तक पहुँचाया।
Meera Bai ने जाति-पांति के बंधनों को तोड़ते हुए यह दिखाया कि प्रेम में “ना घर मेरा, ना घर तेरा” — भगवान सबका है। संत रविदास और कबीर की निराकार भक्ति से प्रेरित होकर, उन्होंने मूर्ति-पूजा में भी अपने व्यक्तिगत अनुभव को सबसे महत्वपूर्ण माना। उनके जीवन के संघर्ष ने यह साबित किया कि सच्चा श्रद्धालु वही है जो उपदेश नहीं, बल्कि अपने अनुभवों के जरिए लोगों को प्रेम के रास्ते पर ले जाता है।
संक्षेप में, Meera Bai ने भक्ति आंदोलन को महिलाओं के दृष्टिकोण, लोक भाषा और व्यक्तिगत अनुभवों से समृद्ध किया। उनका संदेश आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है—भक्ति का असली रूप निडर, सरल और समानता से भरा होता है।
6.4 मीरा बाई की वृंदावन और द्वारका की ओर तीर्थ यात्रा
Meera Bai ने करीब 1524 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ की राजसी दीवारों को छोड़कर वृंदावन की ओर अपना तीर्थ यात्रा शुरू की। वहां उन्होंने रूपा-जीवा गोस्वामी के मठ में ठहरने का फैसला किया। हर सुबह, वे नदियों में स्नान करतीं और रामचरितमानस का पाठ करतीं। निधिवन के पुराने पेड़ों के नीचे, राधा-कृष्ण की लीलाओं को गुनगुनाते हुए, वे बहते पानी में अपनी आत्मा को खो देती थीं।
वृंदावन में Meera Bai का मंदिर, जो चीरघाट के पास है, उनकी साधना का मुख्य केंद्र बन गया। आज भी वहां उनके शालिग्राम-विग्रह की पूजा होती है। भजन-कीर्तन में उनके प्रसिद्ध पद “मेरे तो गिरधर गोपाल…” की गूंज से गोविंद देव, राधा-दमोदर और सप्तदेवालयों का माहौल भक्तिमय हो जाता है।
करीब 1539 ईस्वी में, जब वृंदावन में उनकी आत्मा ने कृष्ण-रस का अनुभव किया, तब वे द्वारका की ओर चल पड़ीं। द्वारका के जगत मंदिर में, जो 15-16वीं सदी में बना है, वहां कृष्ण को “द्वारकाधीश” के रूप में पूजा जाता था। मीरा ने अपने अंतिम वर्ष वहीं बिताए।
कहा जाता है कि द्वारका के उस मंदिर में, जहां उनके पदों की गूंज थी, Meera Bai ने 1547 ईस्वी में कृष्ण की मूर्ति में विलीन होकर अमूल्य समाधि ली। यह एक मधुर प्रेम कहानी थी, जहां प्रेम और परमात्मा का भेद मिट गया। इस तीर्थ यात्रा ने मीरा को संतों की संगत दी और साथ ही लोक-भक्ति साहित्य को वृंदावन और द्वारका की पवित्रता से समृद्ध किया।
6.5 मीरा बाई को विष से मारने की कोशिश
Meera Bai की भक्ति की मजबूती को देखकर उनके ससुराल वालों ने कई तरह के राजसी षड़यंत्र रचे, लेकिन हर बार भगवान कृष्ण की कृपा उनके ऊपर भारी पड़ी। एक बार राणा ने उन्हें फूलों का तोहफा भेजा, जिसमें एक साँप छिपा हुआ था। जैसे ही मीरा ने टोकरी खोली, वह विषैला कोबरा अचानक पवित्र शालिग्राम में बदल गया। यह चमत्कार उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था, कि जो कुछ भी “प्रभु के नाम” आता है, वह चाहे कितना भी विषैला हो, फिर भी अमृत में बदल सकता है।
फिर राणा ने अगली चाल चलते हुए मीरा को “अमृत” कहकर जहर का प्याला भेंट किया। Meera Bai ने पहले उसे प्रभु को अर्पित किया, और फिर खुद उसे पी लिया—और सच में, वह जहर अमृत बन गया। कहा जाता है, जब भी उन्होंने “साँची प्रीत गोविंद से” का उच्चारण किया, उनके संकट धूल की तरह उड़ गए।
इन कहानियों में मीरा की मासूम भक्ति की खूबसूरती झलकती है—जहाँ उनके प्रेम ने दरबारी षड्यंत्रों को भी एक कोमल प्रेम में बदल दिया। उनके अनुभव हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा बाहरी मुश्किलों को पार करके भी हमारे अंदर एक उज्जवल रोशनी जगा सकती है।
7. मीरा बाई की मृत्यु एवं उनके अंतिम पल

संत Meera Bai का जीवन का आखिरी अध्याय भी उनके भक्ति और सरलता से भरा हुआ था, जैसे उनकी रचनाएँ। लगभग 1547 ई. में, जब वे 49 से 59 साल की थीं (इस उम्र पर शोधकर्ताओं में थोड़ी भिन्नता है), मीरा द्वारका की ओर बढ़ीं—वह पवित्र स्थान जहां युवा कृष्ण ने निवास किया था।
जब वे द्वारका पहुँचीं, तो उन्होंने कोई भव्य स्वागत नहीं चाहा। उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई, जहां वे रोज़ प्रभु की झांकी के सामने बैठकर “मेरे तो गिरधर गोपाल…” जैसे भजन गातीं। उनकी सरल मुस्कान और मधुर आवाज ने स्थानीय भक्तों के बीच भक्ति का माहौल बना दिया। कई स्रोतों के अनुसार, इस समय उन्होंने भोग-भंडार से तौबा कर दी और साधारण नमक-रोटी में संतोष किया—उनके अंतिम क्षणों में भी उनका प्रेम अपने मूल रूप में अनमोल बना रहा।
हालांकि हमें उस समय का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन लोककथाएँ एक भावुक पल का चित्रण करती हैं: जब चित्तौड़ से कुछ राजदूत उन्हें वापस लाने आए, तो Meera Bai ने सिर झुकाकर बस इतना कहा, “अब मेरा स्थान यहीं है—जहाँ कृष्ण मेरे पास होते हैं।” कहते हैं, उसी पल उन्होंने अपने प्रिय शालिग्राम-विग्रह में लिपटकर देह त्यागी, और उनका साड़ी जैसा अंगवस्त्र मूर्ति के चारों ओर नतमस्तक मिला।
सच में, हमें 16वीं शताब्दी की कोई समकालीन प्रति नहीं मिलती, लेकिन 17वीं सदी के ग्रंथों में यह कहानी दर्ज हो चुकी थी। इसलिए इतिहासकार चमत्कारिक घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए भी इस बात पर सहमत हैं कि Meera Bai ने अपने अंतिम पल पूर्ण आत्मसमर्पण और अटूट प्रेम में बिताए।
ये क्षण उनके जीवन को खत्म नहीं करते, बल्कि उनके पदों और भजनों को अमर बना देते हैं। आज भी द्वारका के मंदिरों में गूंजता “मेरे तो गिरधर गोपाल…” बताता है कि जब प्रेम सारा जीवन समर्पण से भरा होता है, तो मृत्यु भी एक मधुर मिलन बन जाती है।
8. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न | FAQ
Q.1 Meera Bai कौन थीं?
उत्तर मीरा बाई, जो लगभग 1498 से 1547 के बीच जीवित रहीं, राजस्थान के राठौड़ राजपरिवार में जन्मी एक प्रसिद्ध कवयित्री और कृष्ण की भक्त थीं। उन्होंने अपनी गहरी भक्ति से सामाजिक परंपराओं को चुनौती दी।
Q.2 उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था?
उत्तर मीरा का बचपन काफी कठिनाइयों से भरा था। उनकी माँ का जल्दी निधन हुआ, और मेड़ता के नाना राव दूदा के संरक्षण में उन्होंने कृष्ण की मूर्ति को अपना साथी मान लिया। ये अनुभव उनके भक्ति के रास्ते की नींव बने।
Q.3 विवाह ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया?
उत्तर मीरा का विवाह लगभग 1516 में मेवाड़ के युवराज भोजराज से हुआ। भोजराज ने उन्हें भक्ति में स्वतंत्रता दी, लेकिन राजपरिवार के विरोध का सामना भी करना पड़ा। पति के वियोग और सती प्रथा के दबाव ने उन्हें और भी मजबूत बना दिया।
Q.4 भक्ति की उनकी शैली क्या थी?
उत्तर मीरा की भक्ति में प्रेम और माधुर्य का एक अलग ही रंग था। उन्होंने कृष्ण को अपने “पति” के रूप में मानते हुए सरल और लोकभाषा में पद लिखे, जो भावनाओं से भरे थे।
Q.5 Meera Bai की प्रमुख रचनाएँ कौन-सी हैं?
उत्तर “मीरा-पदावली” में लगभग 100 से 200 प्रमाणित पद शामिल हैं, जिनमें “मेरे तो गिरधर गोपाल…” और “पायो जी मैंने राम-रतन धन पायो” बेहद लोकप्रिय हैं।
Q.6 भजन-कीर्तन में उनका योगदान क्या था?
उत्तर मीरा के मधुर पदों ने ग्रामीण समुदायों में भक्ति-कीर्तन को एक नया रूप दिया। उनकी रचनाएँ ब्रज-भाषा में थीं और उन्होंने भक्ति को जन-उत्सव का हिस्सा बना दिया।
Q.7 क्या उन्होंने सामाजिक बंधन तोड़े?
उत्तर मीरा ने पत्नी होते हुए भी सती प्रथा को ठुकराया और जाति-भेद के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश मानकर समानता की स्थापना की।
Q.8 उनके ससुराल की षड़यन्त्र कथाएँ कैसी हैं?
उत्तर मीरा के ससुराल में कई कहानियाँ हैं जैसे विष-पेय, सांप से भरी टोकरी और कांटों का पलंग भेजने की। लेकिन उन्होंने हमेशा “साँची प्रीत गोविंद से” कहकर हर चुनौती का सामना किया।
Q.9 चरणस्पर्श एवं तीर्थ-यात्राएँ
उत्तर मीरा ने चित्तौड़ से वृंदावन और द्वारका तक तीर्थ-यात्राएँ कीं, जहाँ उन्होंने गोस्वामी और स्थानीय संतों से भक्ति के बारे में चर्चा की।
Q.10 Meera Bai की राग-परंपरा क्या थी?
उत्तर मीरा के पदों को संगीतात्मक पहचान देने वाले राग जैसे कि मल्हार, सोरठा, मंझ और तिलंग हैं, जिन्हें शास्त्रीय और लोक संगीत दोनों में स्वीकार किया गया।
Q.11 उनकी मृत्यु के समय क्या हुआ?
उत्तर कहा जाता है कि मीरा द्वारका के मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में विलीन हो गईं। उनके भजन और समाधिस्थ शालिग्राम आज भी श्रद्धा से पूजे जाते हैं।
Q.12 उनके भक्ति-दर्शन का सार क्या था?
उत्तर मीरा ने भक्ति को कर्मकांडों से अलग करते हुए इसे आत्मा का जीवंत अनुभव माना। उन्होंने व्यक्तिगत अनुभव को सबसे महत्वपूर्ण माना।
Q.13 स्त्री-स्वतंत्रता पर उनका दृष्टिकोण क्या था?
उत्तर मीरा ने कृष्ण के प्रेम को “एकमात्र पति” मानते हुए सामाजिक सीमाओं को पार किया और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया।
Q.14 क्या उन्होंने किसी संत से प्रेरणा ली?
उत्तर मीरा को रैदास और अन्य वैष्णव साधुओं से प्रेरणा मिली। संत रविदास और कबीर की निर्गुण दृष्टि ने भी उन पर गहरा असर डाला।
Q.15 आज के समय में उनका महत्व क्या है?
उत्तर Meera Bai आज भी जन-भक्ति, नारी-सशक्तिकरण और सांप्रदायिक समरसता की प्रतीक हैं। उनके पद आज भी भजन, नृत्य-नाट्य और संगीत कार्यक्रमों में जीवंतता प्रदान करते हैं।
इन्हे भी जरूर पढ़े…
अगर यह आर्टिकल आपको पसंद आया हो. तो इसे अपने दोस्तो के साथ. फेसबुक, वॉट्सएप, इंस्टाग्राम आदि पर जरूर शेयर करे. हमारा फेसबुक पेज.










