Badshah Akbar मुगलों का वह चमकता सितारा माना जाता है. जिसने 13 वर्ष की उम्र में सत्ता संभाली. और भारत के बड़े भू भाग को एकत्र कर संगठित साम्राज्य की नीव रखी.
1 अकबर का परिचय | badshah akbar

badshah akbar, जिन्हें akbar महान कहा जाता है, भारत के सबसे प्रसिद्ध मुग़ल बादशाहों में से एक थे। उनका पूरा नाम अबुल फतेह जलाल उद्दीन मोहम्मद अकबर था।
उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट, जो अब पाकिस्तान में है, में हुआ। उनके पिता हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम थे।
जब badshah akbar सिर्फ तेरह साल के थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया, और उन्हें 1556 में मुग़ल साम्राज्य की कमान संभालनी पड़ी। उस समय साम्राज्य कई मुश्किलों से जूझ रहा था, लेकिन akbar king ने अपनी समझदारी और चतुराई से न केवल इसे स्थिर किया, बल्कि इसे भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े साम्राज्य में बदल दिया।
badshah akbar की गद्दी पर अब बैठने का आरंभ पानीपत की दूसरी लड़ाई से हुआ था, जो 1556 में अफगान सरदार हेमू के खिलाफ लड़ी गई थी। उस लड़ाई में, अकबर ने अपनी सेना की सहायता से जीत हासिल की और मुग़ल सत्ता को पुनः स्थापित किया।
इसके बाद, उन्होंने उत्तरी भारत के कई क्षेत्रों को अपने अधीन किया। मालवा, गुजरात, बंगाल, काबुल, कश्मीर और दक्कन के कुछ हिस्सों को वे जीत लिए, जिससे उनका साम्राज्य बड़ा। उनकी एक विशेषता यह थी कि वे केवल युद्ध से नहीं बल्कि राजनीति, विवाह और संस्कृति के द्वारा भी सफलता प्राप्त करते थे।
उदाहरण के रूप में, उन्होंने आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधा बाई से विवाह किया, जो राजपूतों के साथ उनकी मित्रता का एक नया मार्ग था।
badshah akbar के प्रशासन को बहुत प्रभावशाली माना जाता था। उन्होंने कई नए सुधार किए। उन्होंने ‘मनसबदारी प्रणाली’ शुरू की, जिसमें अधिकारियों को उनकी क्षमता के आधार पर पद दिया जाता था, और उन्हें एक सीमित संख्या में सैनिक रखने की अनुमति थी।
टोडरमल की सहायता से एक स्थायी कर प्रणाली भी आरंभ की गई, जिससे किसानों को राहत मिली और सरकार को नियमित आय होने लगी। धर्म के संबंध में, Emperor Akbar बहुत उदार थे।
उन्होंने सभी धर्मों का समान सम्मान किया और धार्मिक सहिष्णुता के प्रशंसक थे। उन्होंने ‘सुलह-ए-कुल’ की नीति को अपनाया, जिसका मतलब था ‘सबके साथ मेलजोल’। उन्होंने ‘इबादत खाना’ की स्थापना की, जहां वे विभिन्न धर्मों के ज्ञानियों से धर्म, नीति और दर्शन पर चर्चा करते थे।
उन्होंने एक नया धर्म ‘दीन-ए-इलाही’ भी शुरू किया, जिसका लक्ष्य विभिन्न धर्मों की अच्छी बातें एक साथ लाना था। यह धर्म अधिक प्रचलित नहीं हुआ, फिर भी उनकी उदारता का प्रमाण है।
badshah akbar कला और साहित्य के शौकीन थे। उनके दरबार में कलाकार और विद्वान जैसे बीरबल, तानसेन और अबुल फज़ल भी थे। उन्होंने फ़तेहपुर सीकरी नामक शहर बनाया था, जिसमें बुलंद दरवाज़ा और दीवान-ए-आम जैसी अद्भुत इमारतें थीं।
उन्हें संगीत का भी बहुत शौक था और हिन्दुस्तानी शास्त्रीय संगीत को उन्होंने प्रोत्साहित किया। mughal emperor akbar के व्यक्तित्व में एक योद्धा के साथ-साथ समाज सुधारक का भी पहलू था। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, जैसे कि बाल विवाह पर प्रतिबंध और विधवा विवाह को प्रोत्साहन।
उनके न्याय प्रणाली को भी अधिक पारदर्शी और संगठित बनाया गया। badshah akbar की प्रमुख उपलब्धि थी कि उन्होंने भारत के विभिन्न समाजों को एक साथ लाने का प्रयास किया। उनका राज्य धर्म और सांस्कृतिक एकता की पहचान था।
1605 में badshah akbar निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी भारतीय इतिहास में है। उन्होंने सिर्फ सम्राट नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक ऐसे भारत की सोची है जो विविधता में एकता का प्रतीक हो।
2 अकबर का राज्याभिषेक
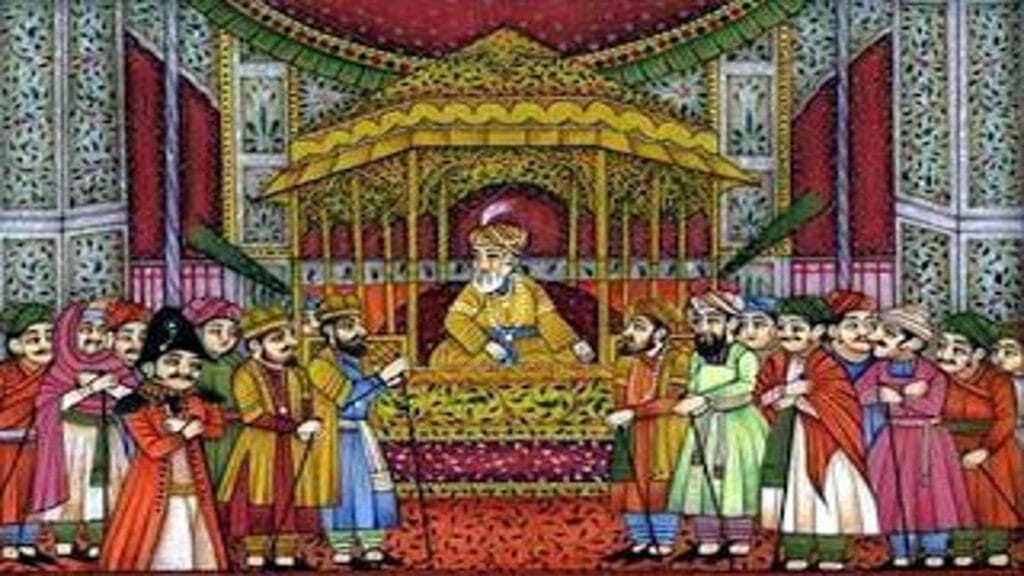
badshah akbar का राज्याभिषेक भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी।
इसमें न केवल मुग़ल साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का मौका था, बल्कि इसने उसे मजबूत किया और विस्तार की दिशा में भी आगे बढ़ा दिया।
यह घटना 14 फरवरी 1556 को हुई थी, जब badshah akbar केवल तेरह साल के थे। उस समय उनके पिता हुमायूं का अचानक निधन हो गया था, जिससे मुग़ल साम्राज्य फिर से मुश्किलात का सामना कर रहा था।
उस समय अंदरूनी कमियों ने उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था और अफगान विद्रोह और राजपूतों का विरोध भी उस समय बढ़ गया था।
इस परिस्थिति में युवा Akbar the Great के लिए तख्त पर बैठना एक चुनौती बन गया था। “पंजाब में राज्याभिषेक कलानौर में हुआ था क्योंकि उस समय अकबर और उनके रक्षक बैरम खान लाहौर में थे।
हुमायूं की मौत भी लाहौर में हुई थी, इसे देखकर बैरम खान ने वहाँ राज्याभिषेक का निर्णय लिया। उसके लिए एक विशेष सिंहासन बनाया गया, जहां badshah akbar को सम्राट घोषित किया गया।”
वह समय बहरम खान के लिए विशेष महत्व रखता था। उन्होंने अपने आप को ‘वकील-ए-सल्तनत’ कहा और badshah akbar की सुरक्षा प्राप्त की। इसके बाद, बहरम खान ने पानीपत के दूसरे युद्ध के लिए तैयारी शुरू की क्योंकि हेम चंद्र विक्रमादित्य ने दिल्ली पर हमला किया था।
badshah akbar के राज्याभिषेक के बाद, मुग़ल सेना ने पानीपत के युद्ध में जीत हासिल की और फिर दिल्ली को फिर से कब्ज़ा किया। इस जीत ने अकबर को वैधता और स्थायिता दी। शुरुआत में बैरम खाँ ने ही वास्तविक ताकत का प्रदर्शन किया, लेकिन अक्बर ने धीरे-धीरे राज्य के दस्ते संभालना शुरू किया।
यह कार्यक्रम चार साल तक चला, फिर Great Akbar ने बैरम खाँ को सम्मान के साथ पद से हटा दिया और खुद शासन करना शुरू किया। राज्याभिषेक के दौरान पारंपरिक मुग़ल रस्में पाली गईं।
badshah akbar ने ताज पहना और फ़ारसी में घोषणा की कि वह अब मुग़ल सम्राट बन गया है। इस अवसर पर कई दरबारी और प्रांतों से आने वाले लोग भी नए सम्राट को बधाई देने आए।
उस दिन अकबर ने लोगों को उपहार दिए, जिससे स्पष्ट हो गया कि एक नया युग शुरु हो चुका है। इतिहासकारों के अनुसार, अकबर का राज्याभिषेक सिर्फ एक समारोह नहीं था, बल्कि यह मुग़ल साम्राज्य की ताकत को दिखाने का एक तरीका था।
इससे यह संदेश गया कि सत्ता का शून्य नहीं बना और साम्राज्य एक सक्षम उत्तराधिकारी के हाथों में सुरक्षित है। अकबर का राज्याभिषेक उसके महान सम्राट बनने की शुरुआत थी।
उस दिन जब एक बच्चा ने ताज पहना तो उसने एक ऐसे शासक का नाम कमाया जोने भारत के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य को परिवर्तित किया।
यह कहानी केवल एक बच्चे की नहीं है, बल्कि एक प्रभावशाली और दूरदर्शी भारतीय इतिहास के एक शासक की है, जिसकी छवि आज भी हमारे इतिहास में गहरी छपी हुई है।
3 अकबर की वीरता
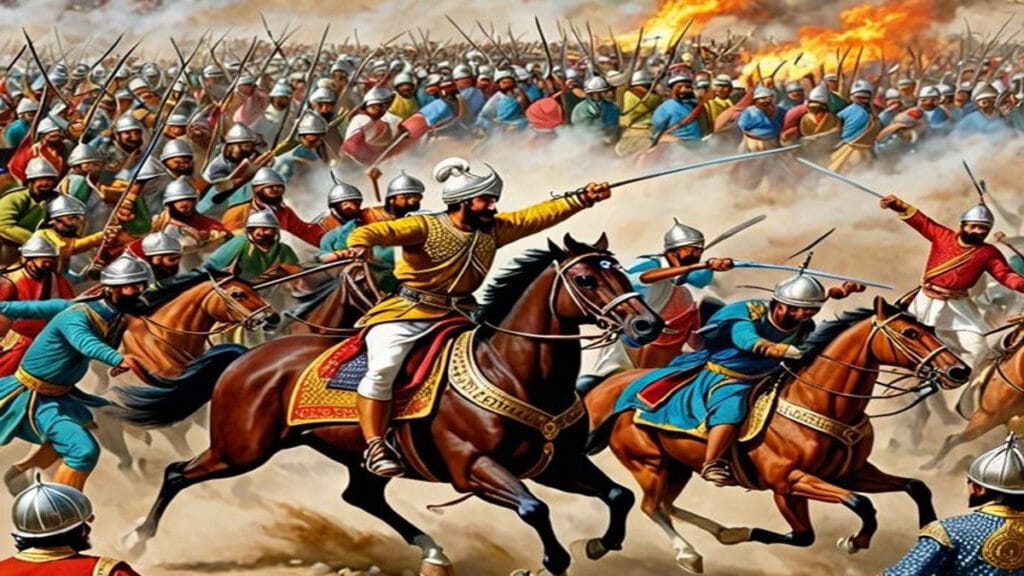
badshah akbar के पराक्रम को भारतीय इतिहास का विशेषांक माना जाता है, जो उसके सिपाही कला, साहस और नेतृत्व के साथ जुड़ा है।
जब वह नवजवान था और ताज का अधिकारी बना, तो उसे न केवल बाहरी दुश्मनों का सामना करना पड़ा बल्कि आंतरिक समस्याओं से भी निपटना पड़ा।
इतनी कम उम्र में मुग़ल साम्राज्य को निर्मित करना एक बड़ी उपलब्धि थी।
उसकी वीरता का पहला उजागर हुआ 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में, जहां उनकी सेना ने अफगान सरदार हेमू को हराया और दिल्ली पर कब्जा किया।
वैराम खाँ की सेना के नेतृत्व में युद्ध होने के बावजूद, अकबर ने अपना धैर्य और उपस्थिति दिखाकर दिखा दिया कि वह मुश्किलों का सामना कर सकता है। अकबर की वीरता सिर्फ युद्ध में तलवार चलाने तक सीमित नहीं थी। उन्होंने युद्धों को केवल खून-खराबा नहीं, बल्कि धैर्य और राजनीति के जरिए जीतने पर भी ध्यान दिया।
जब उन्होंने मालवा, गुजरात, बंगाल और राजस्थान पर अटैक किया, तब यह साबित हुआ कि वे एक कुशल सैन्यकर्मी थे।
गुजरात के दौरान उन्होंने तेज गति से विद्रोहियों को हराया और अहमदाबाद तथा सूरत जैसे क्षेत्रों पर कब्जा किया।
बंगाल में भी उन्होंने मुश्किल हालात में जीत हासिल की। राजस्थान में badshah akbar को उसकी वीरता का और भी बड़ा मौका मिला। उसे चित्तौड़ और रणथंभौर किले जैसे दुर्गों के खिलाफ राजपूत योद्धाओं का सामना करना पड़ा।
चित्तौड़गढ़ किले की लड़ाई उसके लिए एक बड़ा परीक्षण था, जहां उसे अपनी ताकत और राजनीतिक बुद्धि का उपयोग करना पड़ा। राणा उदय सिंह के न होने पर जयमल और पत्ता जैसे योद्धाओं ने दुर्ग की रक्षा की, अकबर ने महीनों तक घेराबंदी की और आखिरकार जयमल को मार गिराया,
जिससे दुर्ग का मनोबल टूट गया। यह साबित करता है कि badshah akbar न केवल एक सम्राट था, बल्कि वह एक योद्धा भी था जो खुद भी लड़ाई में शामिल होता था। जब अकबर ने शांति को भी महत्व दिया, तो उसकी वीरता और भी प्रकट हो गई। उन्होंने आमेर के राजा भारमल की बेटी जोधा बाई से विवाह करके राजपूत समुदाय के साथ मित्रता की राह चुनी।
इससे स्पष्ट होता है कि वीरता का अर्थ सिर्फ युद्ध नहीं है, बल्कि दिल जीतने में भी है। उसने युद्धों को टालने का एक तरीका बनाया और इससे साम्राज्य में स्थिरता और एकता आई।
बैरम खाँ ने विद्रोह किया था, लेकिन badshah akbar ने बिना डरे उसका सामना किया। इससे जाहिर होता है कि उसने सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि असली शक्ति और नेतृत्व के लिए खुद को साबित किया।
जब भी कोई संघर्ष में पीछे हटता, वह हार नहीं मानता था, बल्कि फिर से एकजुट होकर लौटता था। यही उसे अन्य राजाओं से अलग बनाता है। badshah akbar की बहादुरी सिर्फ युद्ध और राजनीति से ही सीमित नहीं थी; वे सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर भी साहसिक निर्णय लेने से हिचकिचाते नहीं थे।
सुलह-ए-कुल की राजनीति जो सभी धर्मों को समान सम्मान देती थी, उस समय की कट्टर सोच के खिलाफ उठाया गया कदम था। उन्होंने धार्मिक संवाद की परंपरा आरंभ की, जिससे विविधता और समर्पण का संदेश फैलाया गया।
इस प्रकार, badshah akbar की पराक्रमता एक विषय है जो कई पहलुओं से संबंधित है, जिसमें युद्ध कला, रणनीति, नैतिक साहस और धार्मिक सहिष्णुता का संगम है। वे केवल एक सेनापति नहीं थे; उन्होंने अपने समय की कठिनाइयों के साथ एक नया भारत बनाने का प्रयास किया।
उनकी पराक्रमता सिर्फ उनकी जीतों से ही नहीं पहचानी जाती है, बल्कि उनके निर्णयों के गहरे प्रभाव से भी। इसी कारण, आज भी अकबर को एक ऐसे शासक के रूप में स्मरण किया जाता है जिनकी पराक्रमता धैर्य और उदारता से परिपूर्ण थी।
4 अकबर का संघर्ष

badshah akbar का युद्ध उसकी महानता का आधार था, जिसने उसे साधारण शासक से भारत का सबसे प्रभावशाली सम्राट बना दिया। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था।
जब वह केवल तेरह साल का था, तब उसे अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद राजगद्दी संभालनी पड़ी। उस समय मुग़ल साम्राज्य कमजोर था। एक ओर, शेरशाह सूरी के वंश ने अफगानों को मुग़लों के खिलाफ उठा दिया था,
और दूसरी ओर, राजपूतों और अन्य स्थानीय शासकों का भी विरोध बढ़ रहा था। इस स्थिति में अकबर का राज्याभिषेक कलानौर में हुआ, जहां उसे नाममात्र का ताज पहनाया गया।
उसकी देखरेख बैरम खाँ कर रहे थे, पर एक बच्चे को असली सत्ता की ओर ले जाना था। यही उसके जीवन की पहली मुश्किल थी। राज्याभिषेक के बाद, उसने हेमू जैसे शक्तिशाली अफगान नेता से युद्ध करना पड़ा, जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था।
दूसरी पानीपत की लड़ाई में मुग़ल सेना की जीत ने उसकी शासनकाल में नई शक्ति देने वाली थी। यह जीत बैरम खाँ द्वारा लाई गई थी, लेकिन badshah akbar ने अपनी बहादुरी से साबित किया कि वह किसी चुनौती से नहीं भागता।
जब उसने धीमे-धीमे बैरम खाँ से सत्ता हासिल करना शुरू किया, तो उसने कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा। बैरम खाँ ने विद्रोह किया, लेकिन अकबर ने उसे परास्त किया और माफ करके उसे छोड़ दिया, जिससे उसकी सहिष्णुता का साक्षात्कार हुआ। इसके बाद, अकबर ने प्रशासन को सही दिशा में लाने के लिए संघर्ष शुरू किया।
वहने कुछ वक्त बाद उत्तर भारत के बिखरे हुए शक्तियों को एकत्र करने और अफगानों के बचे हुए गुटों को दबाने के लिए उसने कठिनाई से देखा।
राजपूतों के प्रतिरोध का सामना किया जो राजस्थान में चित्तौड़ जैसे किलों पर जीत हासिल करना आसान नहीं था।
राणा उदय सिंह और उनके सिपाहियों ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन badshah akbar ने अपनी योजना और धैर्य से इन चुनौतियों को पार किया।
चित्तौड़ के युद्ध में महीनों की घेराबंदी के बाद जीत उसकी इच्छाशक्ति का प्रमाण था। इन सैन्य संघर्षों के साथ, अकबर ने अपने आंतरिक प्रशासन में भी कई परेशानियों का सामना किया।
उसके साम्राज्य में भ्रष्टाचार, अधिकारियों के दर्मियान झगड़े, धार्मिक कट्टरता और लोगों के साथ संवाद की कमी जैसी समस्याएं थीं। अकबर ने इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए कई सुधार किए और एक समाज बनाने की कोशिश की जिसमें धर्म, जाति और वर्ग के बीच की भेदभाव कम हो।
उन्होंने ‘सुलह-ए-कुल’ की नीति अपनाई, जो उस समय में नयी थी। इससे उसे कट्टरवादियों के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने सिद्धांतों पर कभी कमी नहीं की और धार्मिक सहिष्णुता को अपने शासन का मौलिक सिद्धांट बनाया।
उसे गुजरात और बंगाल जैसे क्षेत्रों को अपने अधीन करने में मुश्किल आई। ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से कठिन थे और राजनीतिक दृष्टि से जटिल थे। उसने गुजरात अभियान में लगातार विद्रोहों का सामना किया, परन्तु उसने अपनी सैन्य रणनीति से इनको परास्थित किया।
बंगाल में भी उसे स्थानीय नवाबों के साथ और जलवायु की समस्याओं का सामना करना पड़ा, परन्तु उसने वहां भी जीत हासिल की। badshah akbar का सबसे बड़ा संघर्ष इस प्रकार था कि उसने एक साम्राज्य बनाने का एक योजना बनाई थी, जिससे उसकी सत्ता के साथ-साथ उसकी विचारधारा भी लोगों तक पहुंच सके।
इसलिए उसने कठिनाइयों का सामना करते हुए एक शासन बनाने का प्रयास किया जो न्याय और सहनशीलता पर आधारित था। उन्होंने संघर्ष केवल तलवार से ही नहीं किया, बल्कि संवाद का भी उपयोग किया। उनका इबादतख़ाना, जहां विभिन्न धर्मों के विद्वान मिलते थे, एक बौद्धिक संघर्ष का संकेत था
जो अंधविश्वास और कट्टरता के खिलाफ था। badshah akbar की जीवन यात्रा एक उच्च सेवारत कहानी है, जोने उसे एक महान राजा बनाया। हर कदम पर उसका एक नया चुनौती था, लेकिन उसने कभी हार मानी नहीं।
उसकी इस अद्वितीयता ने उसे एक आदर्श शासक के रूप में इतिहास में स्थानीय दिया। वह सिर्फ युद्धों में ही नहीं जीता, बल्कि अपने भय, बाहरी विरोध और सामाजिक कठिनाइयों से भी लड़ा, जिससे उसने भारत की आत्मा को छूने वाला सम्राट बना।
5 अकबर की युद्धनीति
badshah akbar की जंग करने की रणनीति उसके राज्यातीर्त सबसे महत्वपूर्ण विचारों में से एक थी। इससे केवल उसकी साम्राज्य विस्तार नहीं हुआ बल्कि उसे एक समझदार और विवेकी जनरल के रूप में भी माना गया।
उसके युद्ध की रणनीति में केवल तलवारों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ बल्कि इसमें योजना, राजनीति, चालाकी और प्रशासनिक सहजता का भी समावेश था। अकबर ने मुग़ल सेना को सुधारते हुए इसे बेहतर और संगठित बनाया।
उसने मनसबदारी प्रथा को लागू किया, जिससे सेना में सैनिकों की भर्ती और सैलरी की व्यवस्था सुव्यवस्थित हुई, और इससे सेना में निष्ठा और योग्यता की बढ़ावा मिली। badshah akbar की युद्ध की रणनीति का मूल आधार उसके प्रशासनिक कौशल और भविष्य की क्षमता था।
उन्होंने युद्ध को एक लंबे समय के शासन की योजना के रूप में देखा। हर लड़ाई से पहले, उन्होंने जगह की भौगोलिक स्थिति, विरोधियों की ताकत, स्थानीय समर्थन और अपनी सेना की स्थिति का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। उनकी रणनीति में अचानक हमले, जासूसों का उपयोग और दुश्मनों की कमजोरियों का लाभ शामिल था।
उन्होंने अपने समय के कई मजबूत राज्यों जैसे मालवा, गुजरात, बंगाल और राजस्थान के राजपूतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अधिकांश में जीत हासिल की। राजस्थान में उसकी लड़ाई की रणनीति की एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
उसने चित्तौड़ और रणथंभौर जैसे किलों को जीतने के लिए महीनों तक घेरने की रणनीति अपनाई। चित्तौड़ की लड़ाई में, जब राणा उदयसिंह युद्ध से दूर थे, अकबर ने किले की घंटों तक नाकेबंदी की, रसद के रास्ते को बंद किया और अंत में किले को मजबूर किया। यह उसकी धैर्य और स्थिरता को प्रदर्शित करता है।
रणथंभौर में भी उसने तोपों का सही इस्तेमाल करके किला गिराया। अकबर की रणनीति में एक और महत्वपूर्ण विषय था कि केवल दुश्मन को पराजित करना ही नहीं, बल्कि उसे अपनी कमर में लाना भी। जीतने के बाद जीत हासिल करने वाले शासकों को सम्मानपूर्णता से अपने दरबार में स्वागत करता था
और उन्हें अपनी सरकार के संघर्ष में हिस्सा देता था। इससे विद्रोह की संभावना कम होती थी और लोग उसे एक न्यायप्रिय शासक के रूप में मान लेते थे। राजपूतों के साथ की गई वैवाहिक और राजनीतिक समझौता भी इस नीति का हिस्सा था। उसकी तेज और दूरस्थ रणनीति को गुजरात और बंगाल में भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।
उसने गुजरात में ब्राह्मण्डिक केंद्रों पर हमला करते हुए अहमदाबाद और सूरत में कब्जा जमाया। बंगाल में विजय पाने के लिए, वह दबाव बनाए रखते रहे और अपनी रणनीति में सेना का वितरण और छावनियों का स्थायित्व भी जारी रखा।
badshah akbar ने आधुनिक सैन्य तकनीकों और यूरोपीय बंदूकें का भी इस्तेमाल किया। – अकबर ने आधुनिक सैन्य तकनीकों और यूरोपीय बंदूकों का भी उपयोग किया।
उसने तोपखाने को मजबूत किया और नए हथियारों को शामिल किया, जिससे उसकी सेना की ताकत बढ़ी। – उसने तोपखानों को मजबूत किया और नए हथियारों को शामिल करके अपनी सेना की शक्ति बढ़ाई।
इसके अलावा, उसने युद्ध के दौरान अनुशासन को बेहद जरूरी माना। – साथ ही, उसने युद्ध के समय अनुशासन को बेहद महत्वपूर्ण माना।
अगर कोई सैन्य अभियान सफल नहीं होता या अनुशासन तोड़ता था, तो वह कड़े कदम उठाने में पीछे नहीं हटता, जिससे सेना में अनुशासन बना रहता था। – यदि कोई सैनिक अभियान सफल नहीं होता या अनुशासन को तोड़ता, तो उसे कड़े कदम उठाने में पीछे नहीं हटने देता, जिससे सेना में अनुशासन का पालन होता रहता।
इस प्रकार, badshah akbar की युद्ध की रणनीति न केवल विजय का मार्ग था, बल्कि एक अच्छे संगठित शासन के लिए भी आवश्यक था। उन्हें मालूम था कि स्थायी विजय सिर्फ तलवार से ही नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य, न्याय और उदारता से ही मिलती है।
उनकी रणनीति में शक्ति और साहस के साथ-साथ कूटनीति और समझदारी का संतुलन भी था, जिससे वे अन्य शासकों से अलग थे और उनकी रणनीति को इतिहास में एक आदर्श मानक के रूप में स्थापित किया गया।
6 अकबर द्वारा लड़े गए युद्ध

badshah akbar के शासनकाल में हुई लड़ाइयां सिर्फ भूमि बढ़ाने की कहानियों से कम थीं।
यह उसकी दूरदर्शिता, रणनीति, धैर्य और नेतृत्व की एक स्पष्ट मिसाल थीं। इन युद्धों के दौरान, आकबर की सोच और युद्धकला की नई परिभाषा सामने आई।
उसका पहला बड़ा युद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई थी, जो 1556 में लड़ी गई। यह लड़ाई विशेष थी क्योंकि यह मुग़ल साम्राज्य के अस्तित्व का सवाल था।
उस समय badshah akbar सिर्फ तेरह साल का था और उसका राज का जिम्मा बैरम खान के पास था। उस समय हेमू, एक अफगान सेनापति, दिल्ली पर कब्जा कर चुका था। आकबर ने तुरंत ही अपनी सेना के साथ दिल्ली वापस लेने की कोशिश की और पानीपत में हेमू की ताकत को पराजित कर दिखाया कि मुग़ल साम्राज्य फिर से उभर रहा था।
उस युद्ध के बाद, उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी कि अफगानों और अन्य शासकों से उसके साम्राज्य की सुरक्षा करें और पुनः पहले की तरह बढ़ें।
इसके लिए, उसने मालवा पर हमले करने का निर्णय लिया। 1561 में, उसने मालवा के राजा बाज बहादुर के खिलाफ अभियान चलाया।
बाज बहादुर, जो संगीत में रूचि रखने वाला था, युद्ध में कमजोर था, इसलिए उसकी हार तय थी। badshah akbar की सेना ने उसे पराजित किया और मालवा को अपने साम्राज्य में शामिल किया, लेकिन बाज बहादुर ने विद्रोह किया।
यह युद्ध महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे अकबर को मध्य भारत में प्रवेश का अवसर प्राप्त हुआ। चित्तौड़ और मेवाड़ के बीच कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए। चित्तौड़ की लड़ाई ने अकबर के युद्ध के प्रति धैर्य और सूरति की अच्छी उदाहरण दिया।
राणा उदय सिंह badshah akbar के खिलाफ खड़े रहने का निर्धारण कर चुके थे। अकबर ने चित्तौड़ का दुर्ग घेर लिया, लेकिन जयमल और पट्टा ने सख्ती से मुकाबला किया। अकबर ने कई महीनों तक दुर्ग को घेरा रखा और जितने पर उन्होंने अपनी समर्थ समझ को साबित किया।
अकबर ने अच्छी रणनीति और शक्तिशाली हथियारों की सहायता से रणथंभौर का किला भी जीता, जिसके बाद अन्य किले भी उसके अधीन आ गए।
हल्दीघाटी की लड़ाई badshah akbar और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हुई थी और यह एक महत्वपूर्ण लड़ाई थी। महाराणा प्रताप मुग़ल अधीनता को स्वीकार नहीं करते थे और इस लड़ाई में उनकी बहादुरी का प्रदर्शन हुआ।
अकबर की सेना के काबिल जनरलों ने इस युद्ध में नेतृत्व किया। जबकि युद्ध सामरिक रूप से अकबर की जीत में समाप्त हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप कभी भी पूरी तरह से हार नहीं माने और लगातार संघर्ष किया। ये लड़ाई अकबर और उसके विरोधियों के साहस की प्रशंसा करती है।
इसके बाद badshah akbar ने गुजरात की दिशा में कदम बढ़ाया। गुजरात उस समय व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ के राजा मुजफ्फर शाह तृतीय ने विद्रोह किया था। 1572-73 में अकबर ने खुद गुजरात जाकर विद्रोह को दमन किया और अहमदाबाद, सूरत जैसे शहरों पर कब्जा कर लिया।
यह लड़ाई इस लिहाज से विशेष थी क्योंकि अकबर ने यहां कूटनीति और रणनीति का मिश्रण दर्शाया। बंगाल और बिहार में भी अकबर ने कई युद्ध किए थे।
बंगाल पर नियंत्रण हासिल करना बहुत कठिन था। 1574 में पटना की लड़ाई जीतने के बाद, 1576 तक कई युद्ध हुए। इस क्षेत्र के अंतिम नवाब दाउद खान ने मजबूत प्रतिरोध किया, परन्तु आखिरकार अकबर की योजना और सेना की शक्ति ने इस क्षेत्र को मुग़ल साम्राज्य में शामिल कर दिया।
काबुल और कंधार जैसे सीमाई क्षेत्रों में भी उसे विद्रोहों का सामना करना पड़ा। खासकर काबुल में, जहाँ उसके भाई ने विद्रोह किया था। 1581 में उसे इसे दबाने के लिए वहाँ जाना पड़ा। यह दिखाता है कि badshah akbar हमेशा अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहता था।
इसके अतिरिक्त, उसने सिंध और बलूचिस्तान जैसे क्षेत्रों में भी अभियान चलाए। ये छोटे युद्ध साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षित रखने में मददगार सिद्ध हो गए। दक्षिण भारत के राज्यों की ओर उसका विस्तार उसके राज के समाप्ति के समय शुरू हुआ। उसने अहमदनगर, बीजापुर, और गोलकुंडा पर हमले किए।
हालांकि इनकी पूर्ण सफलता उसके बेटे जहाँगीर के समय में हुई, पर इसकी नींव अकबर ने ही रखी।
इस प्रकार, badshah akbar के युद्ध उसके सम्राट बनने के साथ ही आरंभ हुए और उसकी जीवनी युद्ध और शांति का एक उत्कृष्ट मेल रही थी। इन युद्धों के माध्यम से, उसे न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बड़े साम्राज्य का विस्तार करने का मौका मिला, बल्कि उसने दिखा दिया कि वह केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चा राष्ट्रनिर्माता भी था।
उसकी युद्धनीति में जहां साहस और शक्ति थी, वहीं मेहरबानी और दूरदर्शिता भी थी। इसी संतुलन ने उसके युद्धों को केवल जीत की कहानियों नहीं, बल्कि महान साम्राज्य के निर्माण के स्तम्भ बना दिया।
इसके बाद भी badshah akbar ने दिवेर का युद्ध 1582 में लड़ा. तथा इस युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत और अकबर की बुरी तरह हार हुई. कहा जाता है दिवेर युद्ध के बाद अकबर ने अपने जीवन में कभी भी मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर नही देखा.
7 अकबर का इतिहास
badshah akbar के इतिहास को समझने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति और संस्कृति का बहुत महत्व है। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट (जो अब पाकिस्तान के सिंध में है) में हुआ था।
उनके पिता हुमायूँ थे, जो बाबर के पुत्र और मुग़ल वंश के दूसरे बादशाह थे। अकबर ने अपना बचपन मुश्किलों में बिताया क्योंकि हुमायूँ उस समय निर्वासित थे। उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने जीवन में जो अनुभव हासिल किए, वे उन्हें एक शानदार सम्राट बनाने के लिए काफी थे।
जब उनकी उम्र सिर्फ तेरह साल थी, तब हुमायूँ की मौत हो गई और शासन की जिम्मेदारी उनके संरक्षक बैरम खाँ को सौंपी गई। उसी साल पानीपत में दूसरी लड़ाई में अकबर की सेना ने हेमू को पराजित किया और दिल्ली और आगरा पर मुग़ल फिर से काबू पाया। badshah akbar के पहले कुछ साल बैरम खाँ के मार्गदर्शन में शासन हुआ, लेकिन बाद में उसने खुद सत्ता संभाली।
उसने कई विजयी अभियानों का संचालन किया और मालवा, गुजरात, बंगाल, बिहार, काबुल, कंधार, राजस्थान और मध्य भारत के बड़े हिस्से अपने अधीन कर लिए।
उसने राजपूतों के साथ लड़ाई की, लेकिन कई से संधि और विवाह के जरिए संबंध भी बनाए।
उसका विवाह आमेर के राजा की बेटी जोधा बाई से हुआ, जिससे उसे राजपूतों का समर्थन मिला।
badshah akbar के शासन की खास बात थी उसकी धार्मिक सहिष्णुता।
उसने ‘सुलह-ए-कुल’ नीति अपनाई, जिसमें सभी धर्मों का आदर करने और सभी जातियों के साथ न्याय की बात थी। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में ‘इबादतखाना’ का निर्माण करवाया, जहाँ विभिन्न धर्मों के विद्वान एकत्र होकर चर्चा करते थे।
उन्हें इस मिलनसारता के माहौल में खुद भी नये विचार आने लगे और ‘दीन-ए-इलाही’ जैसी नई धार्मिक विचारधारा की शुरुआत की। इसे ज्यादा प्रसिद्ध नहीं होने मिला और इसकी मौत के बाद यह समाप्त हो गया।
शासन की दृष्टि से भी अकबर का इतिहास प्रेरणादायक है। उन्होंने मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की, जिससे सेना और प्रशासन को संगठित किया गया। इस प्रणाली में अधिकारी को उसकी रैंक और सैनिक संख्या के हिसाब से वेतन और जिम्मेदारी दी गई।
टोडरमल ने विकसित भूमि माप और कर निर्धारण की प्रणाली का मुग़ल प्रशासन में व्यापक उपयोग किया। badshah akbar ने न्याय, शिक्षा, कला और साहित्य को भी प्रोत्साहित किया।
उनके दरबार में अबुल फ़ज़ल, फैजी, बीरबल और तानसेन जैसे ज्ञानियों थे, जिन्होंने उनके शासन को सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर पर ऊंचाई पहुंचाई। अकबर की शासन व्यवस्था धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बन गई थी।
उन्होंने हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया और समाज के सभी वर्गों को शासन में शामिल किया। इसलिए उनका साम्राज्य न केवल भौगोलिक रूप से बढ़ा, बल्कि समाज की नींव भी मजबूत हुई। उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो उस समय में क्रांतिकारी माने जा सकते हैं,
जैसे सती प्रथा को बंद करना, बाल विवाह को रोकना, मंदिरों और गुरुद्वारों की सुरक्षा करना और गैर-मुसलमानों पर जज़िया कर हटाना। ये सभी तथ्य बताते हैं कि अकबर केवल एक विजेता नहीं था, बल्कि एक दूरदर्शी सुधारक और धर्मनिरपेक्ष शासक भी थे।
1605 में badshah akbar की मृत्यु के बाद, उसका साम्राज्य उत्तर से हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक, पश्चिम में सिंध से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला हुआ था। उसकी मृत्यु के बाद, उसका बेटा जहाँगीर सत्ता में आया, लेकिन अकबर द्वारा स्थापित मुग़ल साम्राज्य आगे बढ़ता रहा।
badshah akbar का इतिहास दर्शाता है कि एक शासक केवल ताकत से नहीं, बल्कि अपने विचारों और नीतियों से भी अमर हो सकता है। उसका व्यक्तित्व भारतीय इतिहास में एक ऐसे सम्राट के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने विविधताओं में एकता और समानता के मार्ग को प्रस्तुत किया और अपने शासन को जनता की कल्याण और न्याय की बुनियाद पर स्थापित किया।
7.1 अकबर के नवरत्न
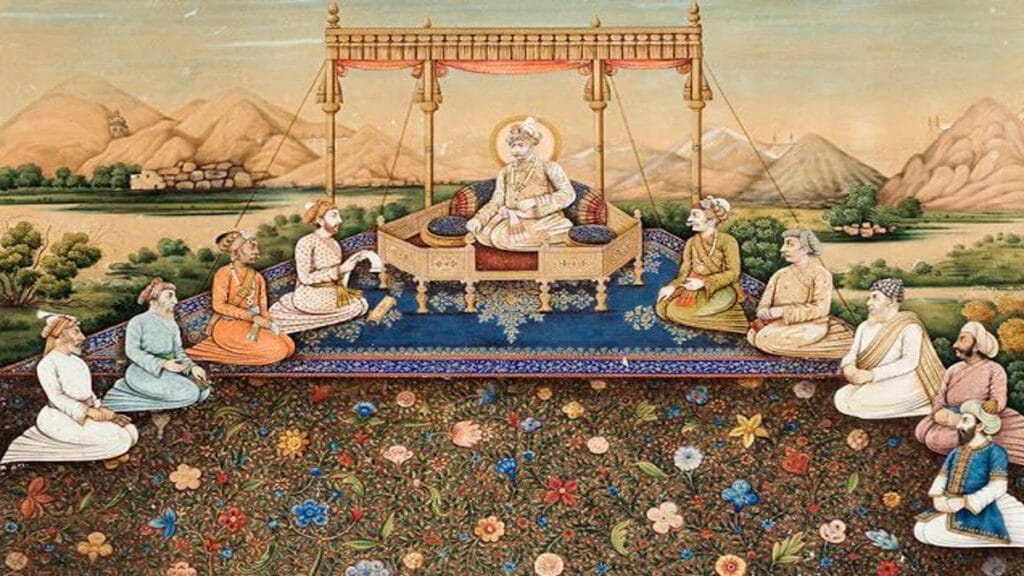
badshah akbar के नवरत्न उसके ज्ञान, सांस्कृतिक रुचि और प्रशासनिक सोच के प्रतीक हैं। ये नौ विशेष व्यक्तियों थे जिन्होंने अकबर के दरबार में अपनी खासियत और सेवाओं की वजह से विशेष जगह बनाई।
ये सभी अपने-अपने क्षेत्र में कुशल थे और उन्होंने अकबर की सरकार को मजबूत और समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाई। जब हम नवरत्नों की बात करते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि ये सिर्फ दरबारी उपाधि नहीं थे, बल्कि वे एक ऐसे स्तंभ थे जिन्होंने राजनीति, साहित्य, संगीत, धर्म, सेना, अर्थव्यवस्था और खगोल विज्ञान में मिलकर मुग़ल दरबार को ऊंचाइयों तक पहुंचाया।
इन नौ रत्नों में अबुल फ़ज़ल का नाम सबसे पहले आता है। वह अकबर के मुख्य सलाहकार और इतिहासवेत्ता था। उन्होंने ‘आइन-ए-अकबरी’ और ‘अकबरनामा’ जैसी पुस्तकें लिखीं, जिनमें अकबर के राजनीतिक और नीतियों का विस्तृत वर्णन है।
वे केवल एक उत्कृष्ट लेखक नहीं थे, बल्कि badshah akbar के विचारों को समझने और उनके प्रवचनों को समझने के लिए भी मशहूर थे, खासकर ‘दीन-ए-इलाही’ के बारे में। उनका भाई फैज़ी भी एक महान कवि था और उन्होंने कई काव्य रचनाएँ कीं, जिनसे अकबर के दरबार में साहित्यिक स्तर मजबूत हुआ।
बीरबल नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध थे। उनका असली नाम महेशदास था। वह अकबर के पास करीबी दोस्त थे और उनकी विवेकपूर्णता और हास्य के लिए मशहूर थे।
उन्होंने मजाक के साथ-साथ badshah akbar को सलाह भी दी। उन्होंने अकबर के धर्मिक सहिष्णुता का समर्थन किया और दीन-ए-इलाही के प्रेरक भी थे। उनकी मृत्यु एक सैन्य कार्यक्रम के दौरान हुई थी, जिससे अकबर बहुत दुखी हुए। तानसेन भी अकबर के नौ रत्नों में शामिल थे।
उन्होंने भारतीय संगीत में महानता हासिल की थी। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ था और वे स्वामी हरिदास के शिष्य थे। तानसेन को यकीन था कि वे अपनी आवाज से बारिश ला सकते थे।
badshah akbar उन्हें ‘मीयाँ तानसेन’ कहकर बुलाते थे। उनके संगीत के आयोजन ने दरबार को नई सांस्कृतिक ऊँचाइयों तक पहुंचाया। राजा टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे और उन्होंने वित्तीय व्यवस्था में सुधार किया।
राजा टोडरमल का पद वित्त मंत्री के रूप में था और उन्होंने आर्थिक संस्थानों में सुधार किया।
उन्होंने भूमि सर्वेक्षण और कर संग्रह की प्रणाली को विकसित किया, जिससे किसान भी सरकार पर भरोसा करने लगे।
उन्होंने भूमि की सर्वेक्षण और कर वसूली की प्रणाली में सुधार किया, जिससे किसान सरकार पर विश्वास करने लग गए।
राजा मानसिंह भी एक महत्वपूर्ण सेनापति थे।
राजा मानसिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी जैसे कि सेनापति।
उन्होंने कई युद्धों का नेतृत्व किया और उनकी निष्ठा और रणनीति के चलते, badshah akbar ने उन्हें उच्च पदों से नवाजा।
उन्होंने कई युद्धों के नेतृत्व किया और उनकी सामर्थ्य और युद्ध रणनीति के कारण, अकबर ने उन्हें उच्च पदों पर बिठाया। मुल्ला अकबर के नौरतनों में दो प्याज़े के रूप में शामिल थे।
उन्हें बुद्धिमान और तेज़ दरबारी माना जाता था। उसकी बीरबल के साथ चर्चा से दरबार में मस्ती का माहौल बना रहता था। सभी इन नौरतनों ने badshah akbar को ऐसा सम्राट बनाया जो सिर्फ युद्ध में विजेता नहीं था, बल्कि विद्या, कला और धर्म का भी प्रोत्साहक था।
इन नवरत्नों के सबसे खास विशेषता थी कि वे विभिन्न धर्मों और जातियों से थे, लेकिन सबने मिलकर काम किया। यह अकबर की समावेशी नीति को प्रकट किया। इन नवरत्नों ने मुग़ल सरकार को एक ऐसा केंद्र बना दिया था
जहाँ से ज्ञान और संस्कृति का प्रसार पूरे उपमहाद्वीप में हुआ। इस प्रकार, badshah akbar के नवरत्न उस युग के सांस्कृतिक और प्रशासनिक उत्कृष्टता की प्रतिकूली भूमिका निभाई और मुग़ल साम्राज्य को स्वर्णकाल बनाने में सहायता पहुंचाई।
7.2 अकबर बीरबल की कहानी
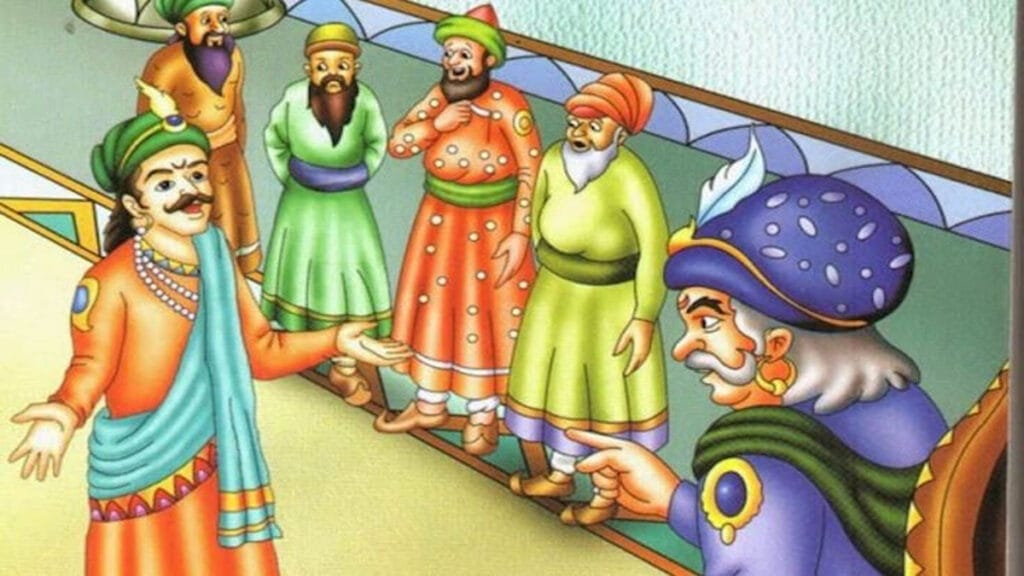
badshah akbar और बीरबल की कहानियाँ भारत का विशेष संपत्ति हैं। ये न केवल रोचक बल्कि नीति, समझदारी और मानवता के महत्व के संदेश भी देती हैं।
अकबर और बीरबल के संबंध केवल बादशाह और दरबार तक ही सीमित नहीं थे; इनमें गहरी मित्रता और विश्वास भी था। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, एक ब्राह्मण परिवार से थे और उनकी समझदारी और हास्यास्पद स्वभाव ने अकबर को इतना प्रभावित किया कि
उन्हें दरबार में उच्च पद पर डाला गया। एक बार अकबर ने बीरबल से यह पूछा कि वह हर सवाल का जवाब कैसे इतनी तेजी से और सही दे देता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्होंने बस सच और तर्क का उपयोग किया है।
एक और कहानी में, जब badshah akbar ने पूछा कि दुनिया में सबसे मीठी चीज़ क्या होती है, तो सभी ने अलग-अलग उत्तर दिए। लेकिन बीरबल ने कहा, “नींद सबसे मीठी होती है,” क्योंकि यह सभी के लिए एक समान होती है।
badshah akbar ने इसे सुनकर मुस्कुराया और बीरबल की समझदारी की सराहना की। एक बार जब अकबर ने पूछा कि किसी की सच्चाई कैसे जानें, तो बीरबल ने उत्तर दिया कि चुप रहने पर चेहरा और आँखें सब कुछ बता देती हैं।
एक दिन, दरबार में चोरी का मामला सामने आया और एक आदमी ने खुद को निर्दोष बताया।
बीरबल ने उस आदमी की आँखों की ओर ध्यान दिया और कहा कि उसका व्यवहार उसके शब्दों से मेल खा रहा है।
उसके बद सहगाने के बावजूद, उसकी बात सच साबित हुई जिससे badshah akbar ने बीरबल की प्रबुद्धता की सराहना की। अकबर ने एक दिलचस्प सवाल पूछा, “इस संसार में कितने तारे हैं?” सब चुप रहे, परंतु बीरबल ने उत्तर दिया, “जितने बाल सम्राट के घोड़े की पूंछ में हैं।”
अकबर ने पूछा कि इसे कैसे साबित करेगा, तो बीरबल ने कहा कि अगर कोई गिन सकता है, तो वह भी कर लेगा। बीरबल की यह बातें उसकी बुद्धिमत्ता को प्रकट करती हैं।
एक दिन badshah akbar ने सोचा कि बीरबल बहुत लोकप्रिय हो रहा है, इसलिए उसे कुछ समय के लिए दरबार से दूर किया। बीरबल ने व्यापारी बनकर शहर में प्रवेश किया और लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता से प्रभावित किया।
जब अकबर को पता चला कि यह व्यापारी वास्तव में बीरबल है, तो उन्होंने समझा कि बीरबल केवल एक दरबारी नहीं, बल्कि लोगों का सच्चा साथी है। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। बीरबल ने कहा कि वह जो बिना सोचे-समझे फैसले लेता है। अकबर मुस्कुरा कर बोले कि यह सच है।
इन कहानियों से साफ है कि बीरबल का काम सिर्फ मजेदार बातें करना नहीं था; वह अकबर के निर्णयों को सही दिशा देने वाला एक गहरी सोच रखने वाला था। एक दिन badshah akbar ने बीरबल से पूछा कि वह क्या कर सकता है ताकि लोग उसकी हमेशा तारीफ करें।
बीरबल ने कहा कि अगर अकबर न्याय प्रिय और दयालु रहेगा तो लोग उसे हमेशा याद करेंगे। एक प्रसिद्ध कहानी में, एक किस्से में अकबर ने बीरबल से कहा कि ऐसा इंसान दिखाएं जो ना तो इस दुनिया का हो और ना ही उस दुनिया का।
बीरबल ने एक गरीब भिखारी को ले आया और कहा कि यह न इस दुनिया का है, क्योंकि इसे रोटी नहीं मिलती और न उस दुनिया का, क्योंकि इसे स्वर्ग की कोई आशा नहीं है।
इस पर badshah akbar प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल को उपहार दिया। यह कहानियाँ सिर्फ राजमहल के बारे में नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन की समस्याओं के उपाय मिलते हैं। बीरबल का चरित्र अभी भी हमारे समाज से जुड़ा हुआ है।
बीरबल ने साबित किया है कि अगर किसी व्यक्ति में समझदारी, मजाक और सचाई हो, तो वह सिर्फ बादशाह का प्रिय बन सकता है, बल्कि लोगों का मार्गदर्शक भी। अकबर और बीरबल की कहानियाँ आज भी लोगों में खुशी और प्रेरणा भरती हैं, और भारतीय कथाओं में उनका नाम हमेशा के लिए महत्वपूर्ण रहेगा।
8 अकबर का निधन
badshah akbar की मौत एक विशेष क्षण था भारतीय इतिहास में, जब एक महान सम्राट अपनी आखिरी सांस ले रहा था। उन्होंने मुग़ल साम्राज्य को मजबूती दी थी। उनके आखिरी दिन इतने शांत थे, जितने महत्वपूर्ण थे उनके पूरे जीवन के लिए।
1605 तक स्पष्ट था कि अकबर बूढ़ा हो रहा था और उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा था। उन्हें दस्त और बुखार की समस्याएं थीं। उस समय, उन्हें ठीक करने के अधिक विकल्प नहीं थे, इसलिए लोग हकीमों और वैद्यों पर आश्रित थे, पर कोई उपाय प्रभावी नहीं रहा।
अकबर ने समझ लिया कि उनका अंत नजदीक है और इसके लिए वे मानसिक रूप से तैयार थे। वे दरबारी लोगों से मिलना कम कर दिया और अकेले समय बिताने लगे। उनके अंतिम दिनों में राज्य के उत्तराधिकारी को लेकर उनकी चिंता बढ़ गई थी।
उन्होंने अपने बेटे सलीम को उत्तराधिकारी बनाने का निर्णय लिया। यह फैसला कठिन था क्योंकि सलीम और अकबर के संबंधों में कई बाधाएं थीं।
badshah akbar ने सोचा कि इस निर्णय से साम्राज्य के लिए सही होगा। अकबर ने अंतिम दिनों में फतेहपुर सीकरी और आगरा के बीच किले में अपनी आखिरी सांसें लीं, जहाँ उनके कुछ करीबी लोग मौजूद रहे।
उनकी आंखों में मौत का भय नहीं था, बल्कि एक प्रकार की शांति प्रगट थी, जैसे कि उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य पूरा कर लिया हो।
उन्होंने भारत में एक सांगठित साम्राज्य स्थापित किया, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और न्याय को महत्व दिया गया। उनकी अंतिम वचनों में एकता और विकास की कामना थी।
उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को सलाह दी कि वह प्रजा को परिवार की तरह समझे और न्याय को सर्वोपरि माने। 27 अक्टूबर 1605 को उनकी मृत्यु हो गई थी।
जैसे-जैसे यह समाचार फैला, पूरे साम्राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। वे हमेशा अपने लोगों को अपने परिवार का हिस्सा समझते थे, जिसके कारण सभी को उनके चले जाने से बड़ा दुःख हुआ।
उनके शासनकाल में हिन्दू-मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन मिला था, इसलिए हर वर्ग के लोग उन्हें याद कर रहे थे। उन्हें सिकंदरा, आगरा में एक भव्य मकबरे में दफनाया गया, जिसे उन्होंने अपने जीवन में बनवाना शुरू किया था और उनके बेटे ने इसे पूरा किया।
यह मकबरा न केवल वास्तुकला के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि एक राजा की याद में है जिन्होंने तर्क और संगठित शासन का निर्माण किया था। अकबर के अंतिम पल न केवल शारीरिक दर्द से भरे थे, बल्कि वे खुद का अवलोकन करने का भी समय था।
उन्होंने अपने जीवन, कील-किश्तों और विवादों पर सोचा।
उन्होंने अपने दोस्तों और सहायकों की मेहनतों को भी याद किया और उनकी महत्वाकांक्षा की प्रशंसा की।
उन्होंने अनुभव किया कि उनकी सबसे बड़ी साफलता सिर्फ अधिकार का विस्तार नहीं था, बल्कि अलग-अलग धर्मों और संस्कृतियों को एक साथ मिलाना था। अकबर की मृत्यु के बाद, जहांगीर ने साम्राज्य की कमान संभाली और अपने पिता की नीतियों को आगे बढ़ाने की कोशिश की।
- badshah akbar का स्थान इतिहास में अद्वितीय रहा, इसलिए उनकी छवि पर जीतना मुश्किल था।
- उनकी मृत्यु ने एक ऐसे युग का अंत किया, जब एक शासक ने शक्ति, बुद्धिमत्ता और इंसानियत को महत्व दिया।
- उनका योगदान साम्राज्य के प्रगति और विकास में अद्वितीय था।
- उनकी छवि एक आदर्श सम्राट के रूप में बनी रही, जिसका योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना। इसलिए, अकबर की मृत्यु सिर्फ एक सम्राट के खत्म होने का ही सामना नहीं था, बल्कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग समाप्त होने जा रहा था।
- उनका जीवन और उनके आखिरी क्षण हमें सिखाते हैं कि एक सच्चा शासक वही है, जो सत्ता का उपयोग समाज के हित के लिए करता है। badshah akbar के अंतिम क्षण न केवल एक घटना थे, बल्कि वे उस विचारधारा की विरासत हैं, जो भिन्नता में एकता और न्याय की महत्वता को समझती है।
अगर यह आर्टिकल आपको पसंद आया हो. तो इसे अपने दोस्तो के साथ. फेसबुक, वॉट्सएप, और इंस्टाग्राम आदि पर जरूर शेयर करे. हमारा कोरा स्पेस पेज.





