पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया. यह युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया. और इस युद्ध के परिणाम क्या थे. यहां जाने पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में
1. पानीपत का तीसरा युद्ध

18वीं सदी का भारत बड़े बदलावों और अस्थिरता से भरा हुआ था। उस समय मुगल साम्राज्य अपने अंतिम दिनों में पहुंच चुका था।
नवाबों और सूबेदारों की महत्वाकांक्षाएं आसमान छू रही थीं, जबकि अफगान आक्रमणकारी भारत के धन पर नजर लगाए हुए थे। इसी बीच, एक नया और ताकतवर हिन्दू साम्राज्य – मराठा शक्ति – भारत की राजनीति में तेजी से उभर रहा था।
इसी स्थिति में 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। यह युद्ध अफगान नेता अहमद शाह अब्दाली और मराठा महासंघ के बीच लड़ा गया, और इसका असर सिर्फ कई हजार लोगों की जान लेने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने भारतीय इतिहास की दिशा को भी बदल दिया।
2. युद्ध की पृष्ठभूमि
पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ने से पहले भारत की राजनीतिक स्थिति बेहद पेचीदा थी। मुगलों का प्रभुत्व पहले ही कमजोर हो चुका था और दिल्ली की सत्ता बस एक नाम रह गई थी। नीचे दक्षिण में, मराठा साम्राज्य बढ़ रहा था और इसका नेतृत्व पेशवा बालाजी बाजीराव कर रहे थे। उनकी सेनाएं मालवा, बुंदेलखंड, दिल्ली और पंजाब तक अपनी सम्पत्ति का विस्तार कर चुकी थीं।
वहीं, पश्चिम में अहमद शाह अब्दाली भारत पर कई बार हमला कर चुका था। उसने 1747 से 1761 के बीच सात बार भारत पर चढ़ाई की। 1757 में दिल्ली पर कब्जा करने के बाद, उसने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रतिनिधि नियुक्त किए।
जब मराठे फिर से पंजाब और दिल्ली पर अधिकार करने लगे, तो अब्दाली ने इसे अपनी शक्ति के लिए चुनौती माना और एक बार फिर पूरी सेना के साथ भारत पर चढ़ाई करने की योजना बनाई।
3. अहमद शाह अब्दाली और उसके सहयोगी
अहमद शाह अब्दाली, जिसे दुर्रानी भी कहा जाता है, अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था। उसकी सेना में अफगान, पश्तून, बलूच, तुर्क, और ताजिक योद्धा शामिल थे।
भारत में उसे कई सहयोगी मिले, जिनमें दिल्ली के रोहिल्ला नेता नजीबुद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और बंगाल के नवाब मीर कासिम शामिल थे। शिया और सुन्नी मतभेदों ने भी उसे कई मुस्लिम नेताओं का समर्थन दिलाने में मदद की।
4. मराठा शक्ति और उसके नायक
पानीपत का तीसरा युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे, जो पेशवा बालाजी बाजीराव के चचेरे भाई थे। उनके साथ कई बहादुर योद्धा जैसे विश्राम बिठ्ठल, जनकोजी शिंदे, मल्हारराव होल्कर, तुकोजी राव, और ईश्वर पंडित थे। पानीपत का तीसरा युद्ध जहां युद्ध के मैदान में लगभग 45,000 प्रशिक्षित मराठा सैनिक मौजूद थे, साथ ही हजारों अनुयायी, व्यापारी, महिलाएं और बच्चे भी थे जो मराठा मुहिम का हिस्सा बने हुए थे।
हालांकि, मराठों की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उन्होंने भारत के अन्य हिन्दू राजाओं, जैसे राजपूतों, जाटों और सिखों को इस संघर्ष में शामिल नहीं किया। राजपूतों ने तटस्थ रहना चुना, जबकि जाटों और सिखों ने अपने-अपने स्वार्थों को प्राथमिकता दी। यही राजनीतिक अलगाव उनकी हार की एक बड़ी वजह बन सका।
5. युद्ध की तैयारी और मार्च
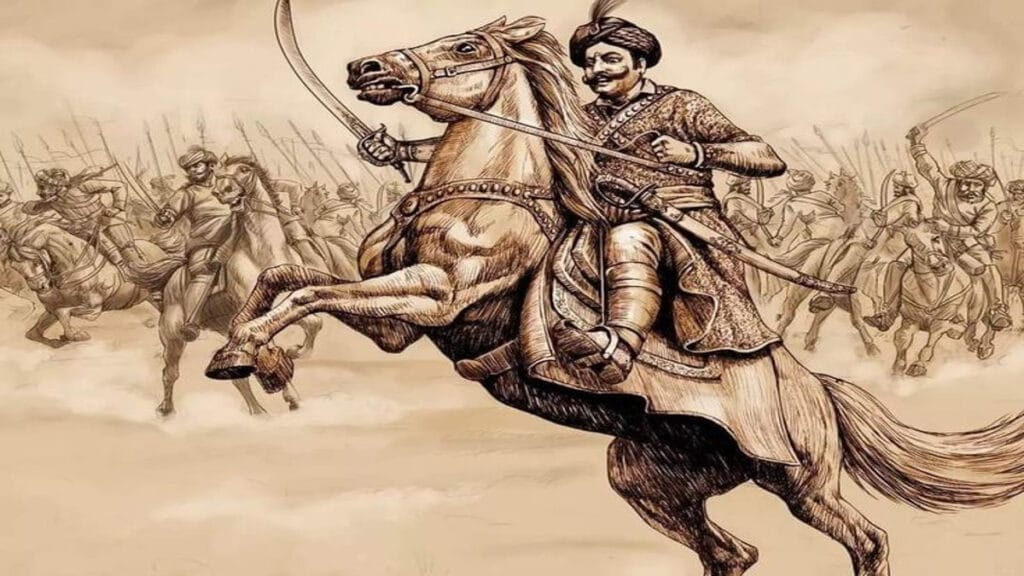
मराठा सेना पुणे से आगे बढ़कर दिल्ली की तरफ रवाना हुई। यह सफर लंबा और मेहनत भरा था। उनके साथ भारी मात्रा में रसद, तोपें, और हथियार थे। यह काफिला पंजाब और हरियाणा तक पहुंचा, जबकि अब्दाली भी दिल्ली की तरफ बढ़ रहा था और कुरुक्षेत्र में पानीपत के नजदीक अपनी सेना इकट्ठा कर रहा था।
पानीपत का मैदान महत्वपूर्ण था, क्योंकि यहां कई बड़े युद्ध लड़े जा चुके थे। वहां एक तरफ यमुना नदी थी, दूसरी ओर रेत के टीले और पीछे की ओर मरुस्थलीय क्षेत्र था। दोनों सेनाएं तैयार थीं, लेकिन मराठे थोड़े देरी से पहुंचे और उन्हें रसद की समस्याओं का सामना करना पड़ा।
6. संघर्ष से पहले की स्थिति
नवंबर 1760 से जनवरी 1761 तक दोनों सेनाएं आमने-सामने रहीं। मराठा शिविर में धीरे-धीरे रसद की कमी होने लगी। अब्दाली की घुड़सवार सेना बेहद तेज और अनुशासित थी, जबकि मराठा सेना में तोप और पैदल सेना की संख्या अधिक थी। सदाशिवराव भाऊ ने अब्दाली से सीधा युद्ध करने की योजना बनाई, जबकि अन्य वरिष्ठ जनरलों ने छापामार रणनीति अपनाने का सुझाव दिया, जिसे ठुकरा दिया गया।
मराठों के पास तोपखाने और इब्राहीम खान की प्रशिक्षित बंदूकधारी टुकड़ी जैसी ताकतें थीं। लेकिन रसद और समय की कमी ने उनके युद्ध की क्षमता को सीमित कर दिया।
7. 14 जनवरी 1761: युद्ध का दिन
14 जनवरी 1761 को, मकर संक्रांति के दिन, दोनों सेनाओं के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अब्दाली की सेना ने पहले पीछे हटने का नाटक किया और मराठा सेना को भ्रमित किया। इब्राहीम खान की तोपें शुरू में अब्दाली की सेना को पीछे धकेलने में सफल रहीं, लेकिन जैसे-जैसे रसद की कमी बढ़ी, मराठों की स्थिति कमजोर होती गई।
सदाशिवराव भाऊ खुद घोड़े पर सवार होकर युद्धभूमि में उतर आए। उनके साथ उनका साहसिक योद्धा विश्वास राव था, जो जल्दी ही युद्ध में मारे गए। मराठा सेनाओं की बहादुरी अद्भुत थी, लेकिन अब्दाली की युद्ध रणनीति और संख्या ने असर डाला।
जब मराठों की पंक्तियाँ टूट गईं, तो अफगान सेना ने शिविर पर हमला किया। इस दौरान स्त्रियों, बच्चों, और नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। हजारों मराठा सैनिकों को बंदी बनाकर दास बना दिया गया। कहा जाता है कि इस युद्ध में एक लाख से अधिक लोग मारे गए, जिनमें अधिकांश मराठा थे।
8. युद्ध का परिणाम

पानीपत का तीसरा युद्ध मराठों की हार के साथ समाप्त हुआ, जो भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक बड़ा झटका था। पेशवा बालाजी बाजीराव, जो पुणे में थे, इस खबर को सही से नहीं झेल सके और कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो गई। मराठा शक्ति को एक गंभीर झटका लगा, और तब तक भारत में एक शक्तिशाली हिन्दू साम्राज्य बनने की उम्मीद भी लगभग समाप्त हो गई।
यद्यपि अब्दाली ने युद्ध जीत लिया, लेकिन वह लंबे समय तक भारत में ठहर नहीं सका। उसे स्थानीय विरोध और रसद की कमी ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। वह भारत में एक स्थायी अफगान राज्य स्थापित नहीं कर सका।
9. भारत पर प्रभाव
पानीपत का तीसरा युद्ध का भारत पर दीर्घकालिक असर पड़ा। एक तो मराठा शक्ति का पतन हुआ, जिससे उत्तर भारत राजनीतिक रूप से बिखर गया। दूसरी ओर, हिन्दू-मुस्लिम शासकों के बीच जो एकता बनने की संभावना थी, वह भी खत्म हो गई।
इपानीपत का तीसरा युद्ध ने भारत को इतना कमजोर कर दिया कि आने वाले वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे-धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर गई।
10. ऐतिहासिक दृष्टिकोण और विश्लेषण
इतिहासकार पानीपत का तीसरा युद्ध को एक बड़ी सैन्य त्रासदी मानते हैं। अगर मराठा सेनाएं होल्कर की सलाह मानकर छापामार युद्ध का तरीका अपनातीं, या अन्य हिन्दू राजाओं को साथ लातीं, तो शायद नतीजे कुछ और होते।
अब्दाली की रणनीति और संगठन उसे जीत दिलाने में मदद की, लेकिन उसके भारत में स्थायी शासन के सपने अधूरे रह गए।
निष्कर्ष
पानीपत का तीसरा युद्ध सिर्फ दो सेनाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति के भविष्य के पुनर्निर्माण की कहानी है। इसने मराठा शक्ति को कमजोर किया और भारत को अंग्रेजी उपनिवेश के लिए तैयार किया।
पानीपत का तीसरा युद्ध हमें यह सिखाता है कि सिर्फ बहादुरी और बलिदान ही नहीं, राजनीतिक समझदारी, कूटनीति और एकता भी बहुत मायने रखती है। पानीपत का तीसरा युद्ध भारत में विदेशी नियंत्रण की एक क्रूर अभिव्यक्ति थी, जिसने भविष्य में कई बड़े बदलावों का मार्ग प्रशस्त किया।
इन्हें भी अवश्य पढ़े…
अगर यह आर्टिकल आपको पसंद आया हो. तो इसे अपने दोस्तो के साथ. फेसबुक, वॉट्सएप, और इंस्टाग्राम आदि पर जरूर शेयर करे. हमारा कोरा स्पेस पेज.

